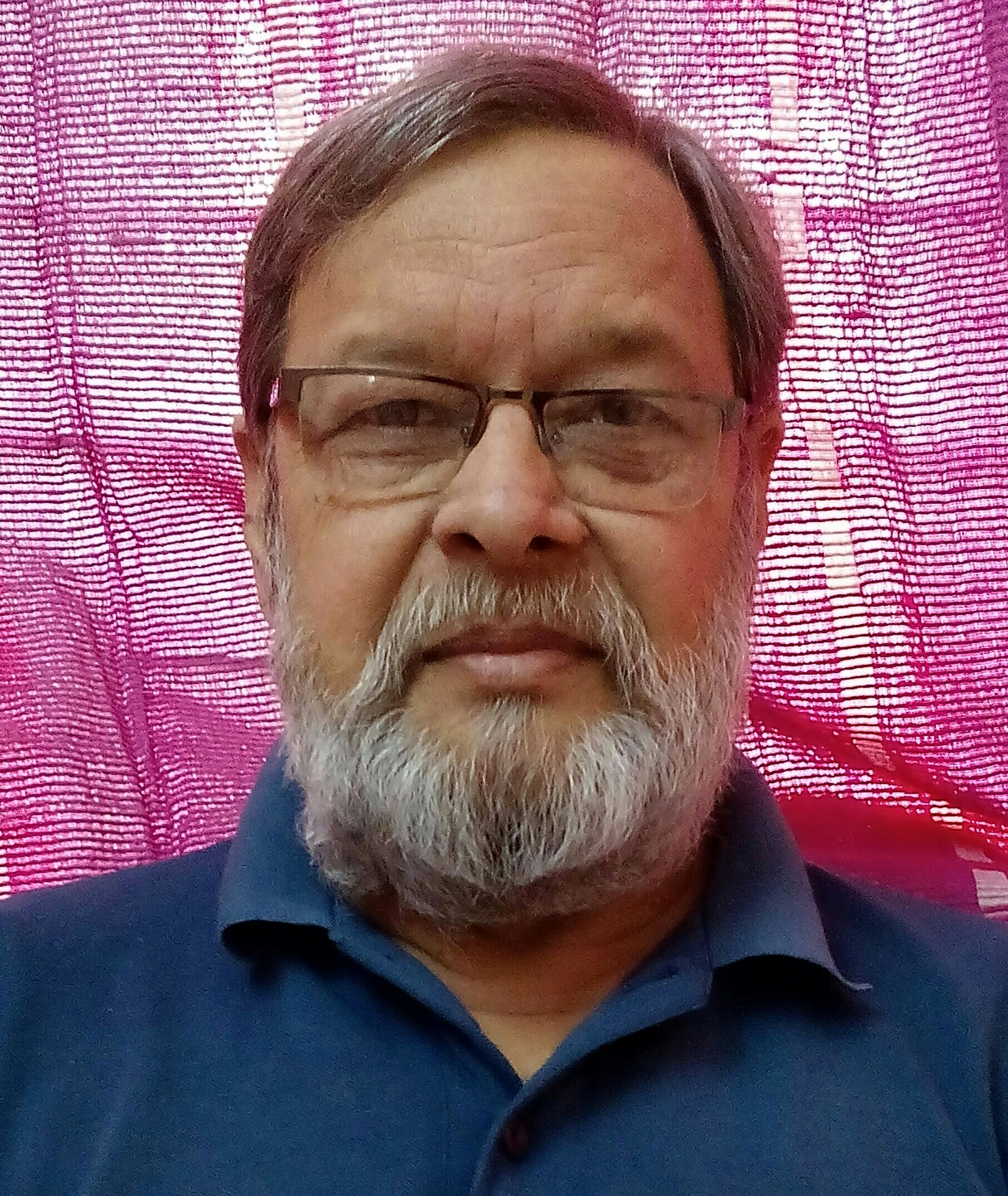
कमजोर और छितरी हुई सांगठनिक, राजनीतिक ताकत को अनदेखा करने की बेशर्म हरकत का ही नतीजा है कि महानगरों में सीवर-लाइन सुधारने वाले सैकडों लोग सालाना जान गंवाते हैं और कोई किसी तरह की चूं भी नहीं करता। यहां तक कि उन्हें मामूली दस्ताने, मास्क और प्राथमिक उपकरण तक नहीं दिए जाते। क्या वापस लौटते प्रवासियों को भोजन कराते हुए हमें इन लोगों का कोई खयाल नहीं आता? क्या हम इतना भी सोच नहीं पाते कि घर भाग रहे मजदूरों की शहर छोडने की वजह केवल बे-रोजगारी, ‘घर की याद’ और ‘असुरक्षा’ भर नहीं हैं? वे दशकों के हमारे इस आमतौर पर लापरवाह और खासतौर पर क्रूर, अमानवीय व्यवहार से भी खिन्न हैं।
थोक में घर लौटते मजदूरों को आखिर फिल्मों में हर अच्छाई को कूटता खलनायक सोनू सूद ही ठीक से समझ पाया। अपने दान-दक्षिणा के साथ-साथ उसने अपने जैसे शहरी मध्यमवर्गीयों को बताया है कि ‘हम मजदूरों को भूल गए हैं’ और ‘उन्हें उनकी पहचान से अलग करके प्रवासी कह रहे हैं।‘ त्रासदी के इस दौर में भी तेल, तम्बाखू और न-जाने क्या-क्या बेचते अमिताभ बच्चनों, सलमान खानों, अक्षय कुमारों और उन जैसे अनेकों के मुंह पर तमाचा मारते हुए सोनू सूद ने याद दिलाया है कि ‘ये वे ही मजदूर हैं जिनकी बनाई सडकों पर हम आमद-रफ्त करते हैं और उनकी बनाई इमारतों में ठाठ से निवास करते हैं।‘ दक्षिण के एक और फिल्मी खलनायक प्रकाश राज और उनके जैसे इक्का-दुक्का नायक, नायिकाओं को छोड दें तो अपनी-अपनी अकूत कमाई का ‘माइक्रोस्कोपिक’ हिस्सा ‘पीएम केयर्स’ में देकर दानवीर बने फिल्मों के महारथियों को दान, दया और दक्षिणा की मार्फत की जाने वाली ‘जन-सेवा’ ही सुहाती रही है। वे अपने-अपने किए-अनकिए पापों की गठरी विसर्जित करने के लिए गरीबों को दान देकर छुट्टी पा लेते हैं, लेकिन कोई सोनू सूद या प्रकाश राज की तरह मजदूरों के दुख-दर्द को समझने की गरज से उनसे संवाद नहीं करता। असल में दान-दक्षिणा एक-तरफा होती है और इससे निपटने के बाद दुबारा मुंह फेरने की जरूरत नहीं रहती। यहां तक कि दान-दाता यह भी जानना नहीं चाहता कि उसके दान का कौन, क्या और कैसे उपयोग कर रहा है।

कडी मशक्कत करते हुए अपने-अपने घर लौटते प्रवासी कहे जाने वाले मजदूरों को ऐसी दया-भावना हर-कोई, हर-कहीं दिखा रहा है। यह दया-भावना नहीं होती तो रास्तों में जान गंवाने वालों की संख्या उससे कई-गुनी ज्यादा होती जिसे सरकार और मीडिया अहर्निश दिखा रहे हैं। लेकिन क्या इतने भर से काम चल जाएगा? क्या मजदूरों के प्रति भलमनसाहत का यह विस्फोट कुछ ऐसा कर सकता है जिससे भागते मजदूरों को ऐसी त्रासदी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल पाए? दया भाव की रौ में दान देकर मुंह फेरने से तो यह कतई संभव नहीं है। ‘स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ (स्वान) के आंकडे बताते हैं कि ‘लॉक डाउन’ के दौर में 99 फीसदी मजदूरों को कोई वेतन नहीं दिया गया, 50 फीसदी के पास एक दिन का राशन बचा था और करीब 64 फीसदी मजदूरों के पास सौ रुपयों से भी कम बचे थे। क्या मजदूरों की यह बदहाली उसी मध्यमवर्ग की ‘मेहरबानी’ से नहीं हुई जो अब दान देने, भोजन करवाने और रास्तों के अन्य इंतजामों में निजी और सार्वजनिक स्तरों पर बढ-चढकर लगा हुआ है? जाहिर है, दान देने वाले हाथों का दमन करने वाले हाथों से कोई रिश्ता–नाता नहीं बचा है। यदि यह संबंध बना, बचा होता तो शहरों में बसा मध्यमवर्ग, सोनू सूद या प्रकाश राज की तरह मजदूरों को, उनके काम को और उनकी अहमियत को पहचान पाता।
नब्बे के दशक के भूमंडलीकरण ने बदहाल ग्रामीण क्षेत्र के छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों को शहरों के औद्योगिक क्षेत्रों की ओर खदेडा था। नतीजे में कुल कामकाजी आबादी का करीब 94 फीसदी इन मजदूरों के बनाए ‘अनौपचारिक क्षेत्र’ से पहचाना जाने लगा। गैर-कृषि क्षेत्र, विशाल सेवा क्षेत्र, ‘वर्कशॉप इंडस्ट्री’ और फुटकर धंधों के जरिए देश का करीब आधा ‘सकल घरेलू उत्पाद’ (जीडीपी) पैदा करने वाले इस ‘अनौपचारिक’ क्षेत्र को शहरों के उद्योगों ने क्या दिया? एक अनुमान के मुताबिक भारत के 95 प्रतिशत उद्योगों में कुल जमा पांच से कम मजदूर स्थायी होते हैं जो ताजा आंकडों के अनुसार अब दो हो गए हैं। जाहिर है, अस्थायी मजदूर को औनी-पौनी मजदूरी, बदहाल काम और रहने की परिस्थितियों और ढेर सारी असुरक्षा से निपटाया जाता है। वर्ष 2014 की ‘बर्कले रिपोर्ट’ के अनुसार शहरों की 35 फीसदी आबादी ‘जीडीपी’ में 70 से 75 प्रतिशत का योगदान करती है, लेकिन बिहार, उत्तरप्रदेश, झारखंड, उडीसा, छत्तीसगढ और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों से आने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था के ‘सेकेंडरी’ और ‘टर्शरी’ क्षेत्रों के इन ‘जीडीपी निर्माताओं’ को शहरों से हमेशा ही सौतेला व्यवहार मिला है। ‘आजीविका ब्यूरो’ के मुताबिक करीब 12 करोड प्रवासी मजदूरों में से चार करोड निर्माण-क्षेत्र, दो करोड घरेलू कामकाज, 1.1 करोड कपडा उद्योग और एक करोड ईंट-भट्टों में रोजगार पाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन-जीने लायक वेतन, काम की बेहतर परिस्थितियां और निवास के लिए सुविधाजनक जगह कभी नहीं दी गई। सवाल है कि क्या मजदूरों पर दया-भाव के चलते भोजन एवं अन्य सामग्री बांटने वालों को इन निर्मम सच्चाइयों पर भी थोडा-बहुत गौर नहीं करना चाहिए?
अपने शहर की सडकों, झुग्गी या मलिन बस्तियों और अक्सर अपराधी या आलसी वृत्ति के कहे जाने वाले लोगों को यदि समझ और संवेदना से देखा जाए तो कोई भी समझ सकता है कि वापसी करते मजदूरों को भोजन कराना एकतरफा दयापूर्ण कृपा की बजाए असल में उनका हक है। राज्य, धर्म, गैर-सरकारी संस्थाओं और जातियों ने बाकायदा सप्रयास हमारी नजरों से उनके योगदान को ओझल कर दिया है। थोडे ध्यान और धीरज से देखें तो आसानी से समझा जा सकता है कि इस मजदूर तबके का शहरों के जीवन में क्या, कितना और कैसा महत्व है, लेकिन आमतौर पर राज्य के विस्तार की तरह काम करने वाले व्यक्ति या संस्थान इस महत्व को अनदेखा ही करते हैं। कमजोर और छितरी हुई सांगठनिक, राजनीतिक ताकत को अनदेखा करने की बेशर्म हरकत का ही नतीजा है कि महानगरों में सीवर-लाइन सुधारने वाले सैकडों लोग सालाना जान गंवाते हैं और कोई किसी तरह की चूं भी नहीं करता। यहां तक कि उन्हें मामूली दस्ताने, मास्क और प्राथमिक उपकरण तक नहीं दिए जाते। क्या वापस लौटते प्रवासियों को भोजन कराते हुए हमें इन लोगों का कोई खयाल नहीं आता? क्या हम इतना भी सोच नहीं पाते कि घर भाग रहे मजदूरों की शहर छोडने की वजह केवल बे-रोजगारी, ‘घर की याद’ और ‘असुरक्षा’ भर नहीं हैं? वे दशकों के हमारे इस आमतौर पर लापरवाह और खासतौर पर क्रूर, अमानवीय व्यवहार से भी खिन्न हैं।
संकट में सक्रिय, उदार और धर्म-भीरू होने की हमारे समाज में पुरानी आदत है, लेकिन क्या यह सक्रियता थोडी आगे बढकर, समाज में साफ दिखाई देती विडंबनाओं को समझने-सुधारने की मशक्कत भी करेगी? करीब 36 साल पहले हुई दुनिया की सर्वाधिक भीषण ’भोपाल गैस कांड’ की त्रासदी हमारा मुंह चिढा रही है, जब हममें से कईयों ने ठीक इसी तरह पीडितों की सेवा में रात-दिन एक कर दिए थे, लेकिन आज तक उस कांड के पीडितों-प्रभावितों को पूरी तरह राहत नहीं मिल सकी और ‘कांड’ का अपराधी पकडा नहीं जा सका। क्या ऐसा माना जा सकता है कि ‘कोविड-19’ काल में सेवा-सुश्रुषा करते हुए हम थोडे बडे, समझदार हो गए हैं और अब शहरीकरण के संकटों पर भी गौर करना शुरु करने वाले हैं। भोजन करने-कराने से निपटकर शहरों में नर्क भोग रही झुग्गी या मलिन बस्तियों का रुख भी कीजिए जहां रहता इंसान कभी-भी घर वापसी की जिद कर सकता है। शहरीकरण की त्रासदियों से निपटने की तजबीज भी यहीं मिलेगी।




























