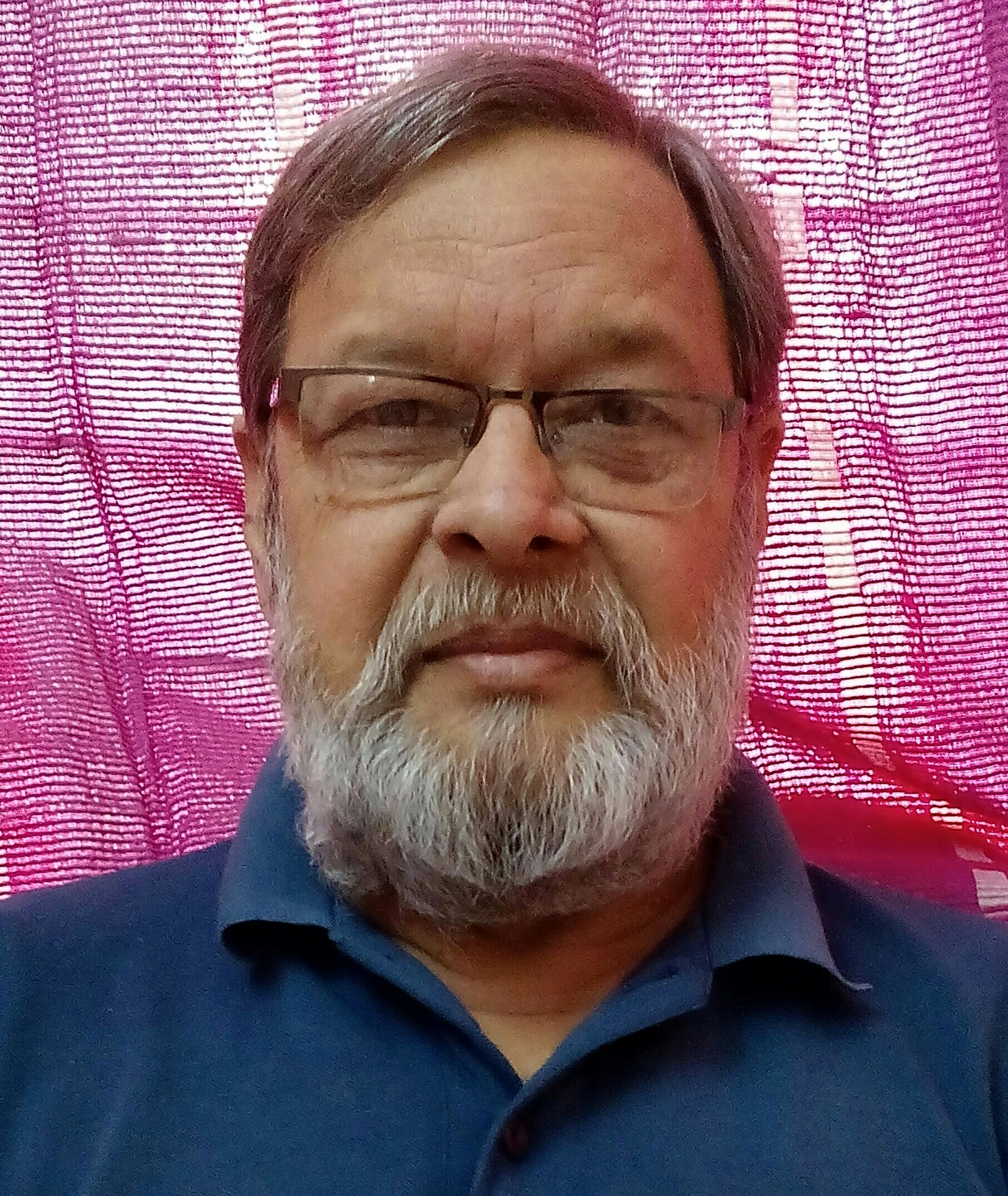
देश की राजधानी की सीमाओं पर बैठे किसानों में यह विभाजन दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन आखिर यह एक ‘आपातकाल’ भर है। बिना किसी बहस-मुबाहिसे के पहले अध्यादेश जारी करके और फिर संसद के दोनों सदनों में पारित करवाकर लाए गए तीनों कानूनों को गौर से देखें तो पता चलता है कि इससे एक हैक्टेयर से कम वाले ‘छोटे,’ एक से दो हैक्टेयर वाले ‘सीमांत,’ दो से पांच हैक्टेयर वाले ‘मध्यम’ और पांच हैक्टेयर से अधिक वाले ‘बडे,’ सभी तरह के किसान प्रभावित होंगे। जरूरत है, इन सभी को आंदोलन में शामिल करने लायक रणनीति की। किसानों को इस व्यापक एकजुटता का आजादी के बाद पहली बार दर्शन हुआ है।
एक तरफ सर्व-शक्तिमान सरकार और दूसरी तरफ देशभर के किसान इन दिनों आमने-सामने मोर्चा बांधकर एक इतिहास भी रच रहे हैं। आजादी के करीब सवा सात दशकों में इस पैमाने का यह दृश्य पहली बार उभरा है। जाहिर है, ऐसे में किसी को किसी का कोई अंदाजा नहीं है। न तो किसान अपनी चुनी हुई सरकार की कारगुजारियों को समझ पा रहे हैं और न ही सरकार अपने किसानों को। नतीजे में एक तरफ, कड़कती सर्दी में करीब तीन हफ्तों से डटे किसानों की खेती के तीनों कानूनों को वापस लेने की गुहार सुनाई देती है तो दूसरी तरफ, निर्णायक नेतृत्व की चुप्पी की पृष्ठभूमि में राज्य और केन्द्र के मंत्रियों, कारकूनों की ऊल-जलूल टिप्पणियां।
इस सबमें एक तीसरा पक्ष भी है, दर्शक नागरिकों का। यह पक्ष उस शहरी मध्यमवर्ग का है जो वकील हरीश साल्वे की मार्फत बड़ी अदालत में दिए जा रहे उन तर्कों से ‘पूरी तरह’ सहमत है जिनके मुताबिक किसानों ने रास्तों पर बैठकर उनके ‘टैक्स’ से चलने वाला आवागमन रोक दिया है और नतीजे में आसपास के इलाकों से होने वाली खाद्य एवं अन्य पदार्थों की आमद ठप्प कर दी है। भूमंडलीकरण के पिछले कुछ सालों तक इस शहरी मध्यमवर्ग पर कोई किसी तरह की उंगली नहीं उठा पाता था। सब जानते थे कि बाजार के पायों पर टिकी भूमंडलीकरण की सम्पन्नता में इसी खरीददार शहरी मध्यमवर्ग ने खासी भूमिका निबाही है। वह भूमंडलीकरण का नियामक बाजार है और इसलिए भले ही उसकी आबादी कुलजमा तीस फीसदी के आसपास हो, किसी को उस पर कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए, लेकिन किसान आंदोलन ने उस पर भी सवाल जड़ दिए हैं।
एक सवाल है, खेती के उत्पाद, गेहूं और शहरी मध्यवर्ग के कर्मचारियों, अधिकारियों की तुलना का। सन् 1970 में जो गेहूं 76 रुपए प्रति क्विंटल था वह आज 1975 रुपए प्रति क्विंटल, यानि करीब 26 गुना हो गया है, लेकिन इसी दौर में केन्द्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह और भत्ते 130 गुना और अध्यापकों का वेतन 320 से 380 गुना तक बढ़ा है। जाहिर है, किसान की आय के मुकाबले शहरी मध्यमवर्ग की आय न सिर्फ कई-कई गुना बढ़ी है, बल्कि और-और बढ़ाए जाने की मांगें भी की जाती रहती हैं। इसकी तुलना में कृषि उत्पादों की कीमतों में मात्र मामूली बढ़ौतरी इसी शहरी मध्यम वर्ग में हाहाकार मचा देती है। क्या दिल्ली की राह रोके बैठे किसानों की मांगों को शहरी मध्यमवर्ग इस तरह से देख सकेगा? क्या वह खेती-किसानी के प्रति अपनी स्वभावगत् चिढ़ को त्यागकर, अपनी आय में उन किसानों का हिस्सा भी जोड़ पाएगा जिसकी मेहनत से उसका पेट भरता है?
हमारे जैसे ‘प्रातिनिधिक लोकतंत्र’ में भले ही संवैधानिक रूप से जिक्र न किया गया हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की खासी अहमियत है। दिल्ली के किसान आंदोलन में सत्ताधारी होने के नाते भाजपा और बरसों से किसानों के साथ संघर्षरत होने के नाते वामपंथियों की उपस्थिति साफ दिखाई देती है, लेकिन देश की बाकी राजनीतिक पार्टियां किसान आंदेालन से दूर क्यों हैं? इसकी एक वजह तो खुद किसान आंदोलन ही है जिसने राजनीतिक पार्टियों को बाकायदा घोषणा करके अपने मंच से दूर रखा है। सवाल है कि क्या इसके बावजूद राजनीतिक पार्टियां इस देशव्यापी आंदोलन को ताकत देने के लिए कुछ नहीं कर सकती थीं? और क्या हमारे संसदीय लोकतंत्र के ढांचे में किसान आंदोलन किसी पार्टी-विहीन राजनीति के जरिए अपने हितों को पूरा करवा सकता है? मौजूदा किसान आंदोलन के जरिए क्या कोई ऐसा तरीका ईजाद नहीं किया जा सकता जिसमें राजनीतिक दल सत्ता और विपक्ष की राजनीति से इतर, देशव्यापी मुद्दों पर भी सक्रिय हो सकें? और कुछ नहीं तो कम-से-कम ‘खालसा एड’ की तरह आंदोलनरत किसानों को थोडी-बहुत राहत ही पहुंचा दें? ध्यान रखें, देश की करीब 67 फीसदी आबादी वाले किसानों ने 1960 से 1990 के बीच अनेक आंदोलन किए हैं, लेकिन किसी राजनीतिक दल ने कभी उनकी मांगों को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया।

सीखने लायक एक बेहद जरूरी बात उस पद्धति की भी है जिसके चलते किसानों को आज चार डिग्री की ठंड में धरना देना पड़ रहा है। कृषि-उत्पादन की मौजूदा पद्धति में लागत या निवेश के मुकाबले उनकी कीमतें बराबर या कहीं-कहीं बेहद कम हैं। ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ (एमएसपी) की दरों को मापदंड मान लें तो लगभग सभी फसलें उससे कम दामों पर बिक रही हैं। धान का ‘एमएसपी’ 1868 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन बिहार में उसे 1100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में बेचा जा रहा है। मक्का का ‘एमएसपी’ 1800 रुपए प्रति क्विंटल है और बिक 800 रुपए प्रति क्विंटल रहा है। मौसम की बेरुखी, आग जैसी दुर्घटनाओं और अन्य व्याधियों से निपटता-सुरझता किसान जब बाजार में अपनी फसलों को लेकर आता है तो उसे लागत के बराबर या कई बार बेहद कम कीमतें मिलती हैं। ऐसे में किसानों को अपनी नैया पार लगाने का एकमात्र तरीका निजी या सरकारी बेंकों का कर्जा भर दिखाई देता है। यह कर्ज ही है जो किसान को अपनी जान तक दांव पर लगाने को मजबूर करता है। पिछले दो-ढाई दशकों में साढ़े चार-पांच लाख किसान इसी कर्ज को चुका पाने की असमर्थता के कारण आत्महत्याएं कर चुके हैं। जाहिर है, ‘हरित क्रांति’ की ‘अधिक लागत से अधिक उत्पादन’ की मौजूदा कृषि-पद्धति को बदलना होगा। आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के लाखों किसानों ने जैविक कृषि अपनाकर खेती की लागत घटाई है और उत्तर, मध्य भारत के ‘हरित क्रांति’ इलाकों के किसानों को भी उनसे सीखना होगा।
सीखने लायक एक और जरूरी बात हर दर्जे के किसानों के एकजुट होने की है। बानगी के तौर पर मौजूदा किसान आंदोलन की सबसे बड़ी मांग ‘एमएसपी’ को ही लें तो 2015 में गठित ‘शांताकुमार समिति’ के मुताबिक इसका लाभ लेने वाले महज छह फीसदी किसान भर हैं। बाकी के 94 फीसद किसान अपनी जरूरतों के अलावा निजी व्यापारियों के भरोसे रहते हैं। ‘राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण’ के मुताबिक 35 फीसदी किसानों ने मंडी में अपना उत्पाद बेचा है, जबकि बाकी के 65 फीसदी किसानों ने निजी व्यापारियों को बिक्री की है। किसानों के बीच का यह विभाजन बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल सरीखे राज्यों और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे उन राज्यों के बीच भी है जिनके पास औसत से अधिक जमीन है और जो बड़े और मध्यम श्रेणी में आते हैं। बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल सरीखे राज्यों में किसानों की जोत का आकार छोटा और सीमांत है।
देश की राजधानी की सीमाओं पर बैठे किसानों में यह विभाजन दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन आखिर यह एक ‘आपातकाल’ भर है। बिना किसी बहस-मुबाहिसे के पहले अध्यादेश जारी करके और फिर संसद के दोनों सदनों में पारित करवाकर लाए गए तीनों कानूनों को गौर से देखें तो पता चलता है कि इससे एक हैक्टेयर से कम वाले ‘छोटे,’ एक से दो हैक्टेयर वाले ‘सीमांत,’ दो से पांच हैक्टेयर वाले ‘मध्यम’ और पांच हैक्टेयर से अधिक वाले ‘बडे,’ सभी तरह के किसान प्रभावित होंगे। जरूरत है, इन सभी को आंदोलन में शामिल करने लायक रणनीति की। किसानों को इस व्यापक एकजुटता का आजादी के बाद पहली बार दर्शन हुआ है। जरूरी है, इस मौके का फायदा उठाते हुए बुनियादी मुद्दों पर भी चर्चा कर लेना। (सप्रेस)
































