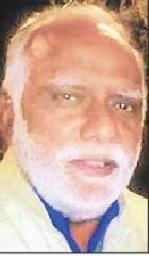
संवाद के लिए बनी भाषा आजकल फिरकापरस्ती की दुनाली बनती जा रही है। सत्ता पर विराजी भाजपा अपनी एक-आयामी नजर से खुद को छोड़कर बाकी सबको खारिज करने में लगी है। उर्दू को एक धर्म-विशेष की भाषा करार देना इसी इकहरी नजर की बानगी है। क्या हैं, इसके निहितार्थ?
आजकल भाई लोग चुटिया बाँध, जनेऊ कसकर उर्दू के पीछे पड़े हैं। भाषा के आधार पर अपना पुराना नफरती राग फिर से अलापना शुरू कर दिया है। उर्दू, जिसे मुसलमानों की भाषा करार दिया जा रहा है, वह ठेठ हिन्दुस्तानी है जो हिंदवी, रेख़्ता, उर्दू जैसे नामों के साथ धरती के इसी हिस्से पर जन्मी, पली, जवान हुई और आज भी बूढ़ी होने को राजी नहीं है !! वह उसके एक बड़े हिस्से, खासतौर से हिंदी, मराठी और बांग्ला भाषाई इलाकों की बोलचाल का हिस्सा बन चुकी है ; इस कदर कि उसके खिलाफ बोलने वालों को भी उसी भाषा से शब्द लेने पड़ते हैं।
उन्हें नहीं पता कि उर्दू मुसलमानों की जुबान नहीं है! कोई भी हिन्दुस्तानी इसे या किसी भी दूसरी भाषा को किसी धार्मिक सम्प्रदाय के नाम करने के लिए क़तई राज़ी नहीं हो सकता। यूं भी भाषा किसी धर्म, संप्रदाय, जाति की नहीं होती। वह कई मर्तबा इलाक़ाई होती है, जैसे बांग्ला, मराठी, गुजराती आदि भाषाएं हैं, मगर हिन्दी-उर्दू उस तरह की भाषाएँ नहीं हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जहां-जहां हिंदी है वहां-वहां उर्दू है और जहां-जहां उर्दू है वहां उसकी हमजोली हिन्दी है। इसलिए इनके संगम को सदा गंगा-जमुनी कहा और माना गया है। दिलचस्प है कि दोनों का नाभि-नाल संबंध अमीर ख़ुसरो से है और दोनों का पालना बृज और अवधी का रहा है।
उर्दू प्रेमचंद, आनंद नारायण मुल्ला, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त, रघुपति सहाय फ़िराक़ गोरखपुरी, सरदार भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, राजिन्दर सिंह बेदी, सरदार रतन सिंह, जगन्नाथ आज़ाद, प्रोफ़ेसर ज्ञानचंद जैन, बलबीर सिंह रंग और गोपीचंद नारंग की भाषा है। क्या इनके अदब को कोई नफरती अज्ञानी अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक ख़ानों में बांट सकता है? क्या विख्यात कवियों – शमशेर बहादुर सिंह और त्रिलोचन शास्त्री द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू शब्दकोश के लिए दी गई ख़िदमात को नकारा जा सकता है? शमशेर जी ने तो अपने समय की प्रखर पत्रिका ‘दिनमान’ में ‘उर्दू कैसे सीखें’ जैसे कॉलम चलाए थे जिससे प्रभावित होकर कई लोग उर्दू में आए।
क्या प्रकाश पंडित के योगदान को भुलाया जा सकता है जिन्होंने सारे प्रमुख शायरों की रचनाओं को संपादित कर हिन्दी जगत को सौंपा और कई पीढ़ियों को उर्दू के प्रति जागरूक बनाया। उर्दू किशन चंदर और किशन तलवानी की भाषा रही। गुलज़ार से लेकर क़मर जलालाबादी, नक़्श लायलपुरी और रजिन्दर किशन जैसे नामों से फ़िल्मी दुनिया गुलज़ार हुई पड़ी है। कृष्ण बिहारी नूर और शीन क़ाफ़ निज़ाम (मूल नाम श्रीकृष्ण) जैसे नाम शीर्षस्थ उर्दू शायरों में शुमार हैं। ऐसे उदाहरणों से ज़ाहिर हो जाता है कि उर्दू सबकी है, सिर्फ़ मुसलमानों की नहीं। उसे अल्पसंख्यकों की भाषा बनाकर उसका प्रभाव व आयतन कम करना एक क्षुद्र साम्प्रदायिक क़िस्म की हरकत है।
काज़ी अब्दुल सत्तार, डॉ. मोहम्मद हसन, प्रो. नईम, प्रो. आफ़ाक़ अहमद, ‘जनवादी लेखक संघ’ को हिन्दी-उर्दू लेखकों का संगठन बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ‘जनवादी लेखक संघ, मप्र’ के अध्यक्ष रहे प्रो. आफ़ाक़ अहमद ने कराची के उर्दू अधिवेशन में गर्व से कहा था कि उर्दू इसलिए हिन्दुस्तान का मुक़द्दर नहीं बनी है कि उसे मुसलमान बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि बहुसंख्यक हिन्दू उससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जिन्हें अमीर ख़ुसरो, जायसी, ग़ालिब और इक़बाल उतने ही प्यारे हैं जितने कि कालिदास, तुलसी, सूर, मीरा या निराला।
हिन्दी ही नहीं उर्दू साहित्य के इतिहास में भी उर्दू को कभी अल्पसंख्यकों या मुसलमानों की भाषा नहीं बताया गया और न किसी स्कूल या कालेज में ऐसा पढ़ाया गया। उर्दू एक सेक्युलर, धर्म और पंथ निरपेक्ष भाषा है और जो लोग उर्दू को धर्म विशेष से जोड़ रहे हैं वे सिर्फ उर्दू का ही नुक्सान नहीं कर रहे, बल्कि हिंदी के साथ भी उन्होंने यही सलूक किया है। उनका इरादा हिंदी के हिन्दुत्वीकरण का है। स्वीकार्य तो उन्हें हिंदी भी पूरी तरह से नहीं है, उनके हिसाब से धरा के इस हिस्से की एक ही भाषा है जो उन्हें भाती है और वह संस्कृत है जो खुद उनकी समझ में नहीं आती।
साल 2011 की जनगणना में 24,821 लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा बताया था। यह भारत की कुल आबादी का 0.00198 प्रतिशत है। इनका भी काफी बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में पाया जाता है। संस्कृत की यह गत इसे धर्म के साथ नत्थी करने से हुयी। पहले इसे ‘देव भाषा’ बताया गया और उसके बाद इसे पढ़ने, इसे बरतने का विशेषाधिकार चंद लोगों, ब्राह्मणों में भी उच्चकुलीन माने जाने वालों तक सीमित कर दिया गया। भले ही आज हिंदी की बात हो रही है, मगर जर्मनी के नाज़ियों और इटली के फासिस्टों से ली ‘एक भाषा – एक नस्ल – एक संस्कृति – एक धर्म’ की भौंडी समझदारी का समाहार हिंदी में नहीं, संस्कृत में किया जाना है।
सावरकर ने मराठी से उर्दू और फारसी के शब्दों को विलोपित करने का एक पूरा अभियान चलाया था, लेकिन मराठी-भाषियों ने उसे तवज्जोह नहीं दी थी। इधर हिंदी में भी यही प्रयत्न किये जाते रहे हैं – उसमें से हिन्दुस्तानी के शब्द हटाकर संस्कृतनिष्ठ बनाये जाने की योजना है जिसका एक उदाहरण राजस्थान का वह स्कूल है जहां ‘विदाई समारोह’ को ‘फेयरवेल पार्टी’ कहना स्वीकार है, खालिस भारतीय भाषा का ‘जश्न-ए-अलविदा’ अपराध लगता है। इस हिसाब से भारत के कई हजार वर्षों के इतिहास में इनका स्वर्णिम रोलमॉडल पेशवा-शाही है, जिसके दोनों ही शब्द फारसी के हैं।
उर्दू या हिंदी – या और किसी भी भाषा को – किसी धर्म विशेष से बांधना उसके धृतराष्ट्र-आलिंगन के सिवा और कुछ नहीं। ऐसे तत्वों की एक सार्वत्रिक विशेषता है ; वे न हिंदी ठीक तरह से जानते हैं न हिंदी के बारे में कुछ जानते हैं। उन्हें नहीं पता कि हिंदी की पहली कहानी “रानी केतकी” लिखने वाले मुंशी इंशा अल्ला खां थे। पहली कविता “संदेश रासक” लिखने वाले कवि अब्दुर्रहमान – पहले लोकप्रिय कवि और हिन्दवी, जिससे हिंदी और रेख्ता दोनों निकलीं, के बनाने वाले अमीर खुसरो थे, पहला खण्डकाव्य लिखने वाले मलिक मोहम्मद जायसी थे। इन्हीं की कृति थी ; ‘पद्मावत,’ जिस पर कुछ साल पहले रार ठानी गई थी। हिंदी में पहला शोधग्रंथ -पीएचडी – फादर कामिल बुल्के का था। ये वे ही हैं जिन्होंने ‘हिंदी शब्दकोष’ तैयार किया था। प्रथम महिला कहानी लेखिका बंगभाषी राजेन्द्र बाला घोष थीं जिन्होंने “दुलाई वाली” कहानी लिखी। कई ग्रंथों के हिंदी अनुवाद के माध्यम बने राममोहन राय बंगाली भी थे और ‘ब्रह्मोसमाजी’ भी।
साहित्य सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचन्द ने इसी तरह के बहकावे में आये अपने मुसलमान दोस्तों के लिए लिखते हुए जो दर्ज किया था आज वही बात खुद को हिंदी-भक्त कहने वालों के लिए भी कही जा सकती है। उन्होंने कहा था कि “मेरा सारा जीवन उर्दू की सेवकाई करते गुज़रा है और अब भी मैं जितना उर्दू लिखता हूँ, उतनी हिंदी नहीं लिखता। कायस्थ होने और बचपन से फ़ारसी का अभ्यास होने के कारण उर्दू मेरे लिए जितनी स्वाभाविक है, उतनी हिंदी नहीं। मैं पूछता हूँ, आप इसे हिंदी की गर्दनज़दनी (गर्दन, कंधे का दर्द) समझते हैं? क्या आपको मालूम है, और नहीं है तो होना चाहिए, कि हिंदी का सबसे पहला शायर, जिसने हिंदी का साहित्यिक बीज बोया था, वह अमीर खुसरो था?”
मुंशी प्रेमचंद आगे लिखते हैं कि “क्या आपको मालूम है, कम-से-कम पाँच सौ मुसलमान शायरों ने हिंदी को अपनी कविता से धनी बनाया है, जिनमें कई तो चोटी के शायर हैं। क्या आपको मालूम है, अकबर, जहाँगीर और औरंगज़ेब तक हिंदी की कविता का शौक रखते थे और औरंगज़ेब ने ही आमों की दो नस्लों का नाम ‘सुधा-रस’ और ‘रसना विलास’ रखा था। क्या आपको मालूम है, आज भी हसरत और हफ़ीज़ जालंधरी जैसे कवि कभी-कभी हिंदी में ताबाआज़माई (विमर्श में नयापन) करते हैं? क्या आपको मालूम है, हिंदी में हज़ारों शब्द, हज़ारों क्रियाएँ अरबी और फ़ारसी से आई हैं, इसीलिए हिंदी और ‘उर्दू’ की सारी-की-सारी क्रियायें एक हैं और क्रियायें ही भाषा की पहचान तय करती हैं, संज्ञा और विशेषण नहीं, जो एक भाषा से दूसरी भाषा में घूमते रहते हैं। अगर यह मालूम होने पर भी आप हिंदी को उर्दू से अलग समझते हैं, तो आप देश के साथ और अपने साथ बेइंसाफ़ी करते हैं…..”
जो जेहनियत आज उर्दू के बारे में नफरती जुबान इस्तेमाल कर रही है वही हिंदी पर भी हमलावर बनी हुई। अतिशुध्द बनाने, संस्कृतकरण करने के जुनून में उसे इतनी क्लिष्ट और हास्यास्पद बनाया जा रहा है कि वह किसी की समझ में नहीं आती। यह ऐसा मनोरोग है जो निज भाषा से प्यार का मतलब बाकी भाषाओं के तिरस्कार तक पहुंचा देता है। दूसरे को निकृष्ट मानकर रखना एक तरह की हीन ग्रंथि है – मनोरोग है। हर भाषा का अपना उद्गम है, सौंदर्य है, आकर्षण है, उनकी मौलिक अंतर्निहित शक्ति है। बाकी को कमतर समझने की यह आत्ममुग्धता दास-भाव भी जगाती है। यही दास-भाव है जो अंग्रेजी की घुसपैठ को तो माथे का चन्दन बनाता है, मगर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, असमी, कश्मीरी, खासी-गारो-गोंडी-कोरकू, भीली, मुण्डा, निमाड़ी आदि को अस्पृश्य बना देता है। इसी विकृति का एक रूप विस्तारवादी है जो ब्रज, भोजपुरी, अवधी, बघेली, मैथिली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी, मगही, मारवाड़ी, मालवी को भाषा ही नहीं मानता। अब भला ये हिंदी की शाखा या उपशाखा कैसे हो गयीं, जबकि हिंदी आधुनिक है और ये उसकी परदादी और परनानी की भी परदादी और परनानियाँ हैं। (सप्रेस)
































