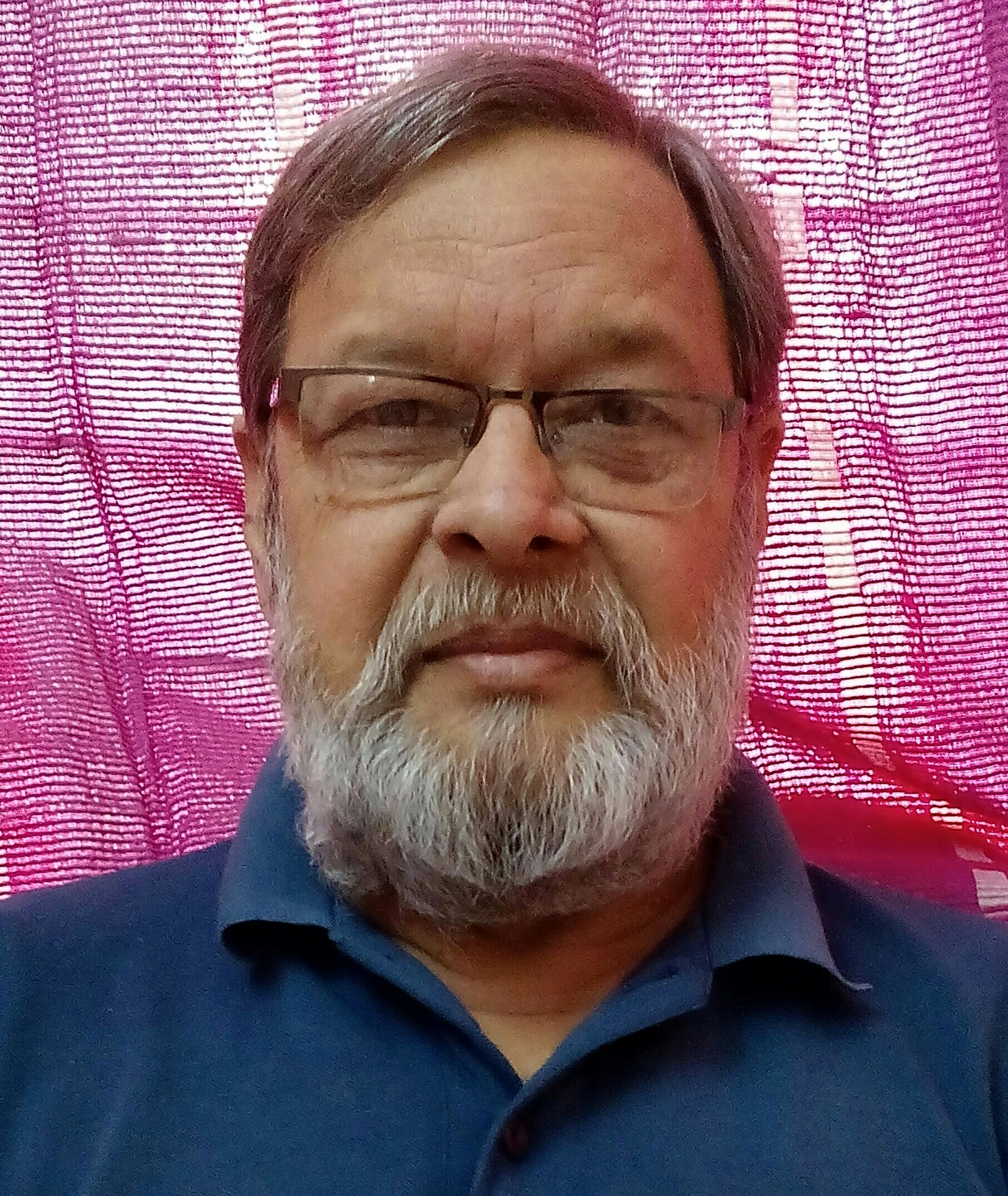
वैसे देखा जाए तो बकासुर की यह कथा विज्ञान और तकनीक पर न्यौछावर विद्वानों से लेकर अहर्निश भक्तिभाव में डूबे धर्म-प्राणों तक सभी में कमोबेश मौजूद रहती है। सभी को लगता है कि संकट या समस्या का एकमात्र इलाज केवल उनके पास ही मौजूद है। मौजूदा किसान आंदोलन को ही देखें तो जहां सरकार को लगता है कि दो नए कानूनों को रचकर और तीसरे का संशोधन करके उसने सात दशकों की किसानों की समस्याओं को निपटा दिया है
किसान आंदोलन पर सुप्रीमकोर्ट की ‘तजबीज’ ने एक बार फिर महाभारत के उस राक्षस बकासुर की कहानी ताजा कर दी है जिसमें संकट पैदा करने वाले से ही संकट के निदान की आशा की जाती है। कहानी में बकासुर अपने भोजन के निमित्त रोज एक मनुष्य का वध किया करता था। हर दिन सुबह गांव के लोग इस आशंका में डरे-सहमे रहते थे कि पता नहीं कब उनका नंबर आ जाए। ऐसे में कुछ समझदार लोगों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने बकासुर से निवेदन किया कि ‘महाराज, आप रोज गांव तक आने का कष्ट करते हैं इसलिए अब से हम आपकी सेवा में व्यवस्थित रूप से एक मनुष्य और पानी खुद ही भेज दिया करेंगे। आपको घर बैठे भोजन-पानी मिल जाने के अलावा इस तरकीब से सबका रोज-रोज का वह डर भी खत्म हो जाएगा जिसके चलते हम सुबह से अपना नंबर आने के डर से कांपते रहते हैं।
बकासुर से निपटने की इसी तर्ज पर सुप्रीमकोर्ट ने मौजूदा किसान आंदोलन से निपटने का खाका खींचा है। दो नए कानूनों और एक पुराने कानून में संशोधन को खारिज करवाने की खातिर पिछले 54-55 दिनों से दिल्ली की सीमाओं को घेरकर बैठे किसानों के आंदोलन के लिए बडी अदालत ने देश के चार नामी-गिरामी लोगों की समिति गठित करके मामले को सुलझाने का प्रस्ताव रखा है। कृषि-अर्थशास्त्री डॉ.प्रमोद कुमार जोशी और डॉ. अशोक गुलाटी, महाराष्ट्र के ‘शेतकरी संगठन’ के अनिल घनावट और पंजाब के किसान नेता भूपिन्दर सिंह मान घोषित रूप से विवादित कानूनों के समर्थक रहे हैं। इनमें से कईयों ने कानून की जरूरत पर अखबारों में लिखा है और कई सीधे सरकार के पास जाकर अपनी सहमति दर्ज करवा आए हैं। इनमें से मान साहब ने, अपने संगठन से गरियाए और निकाले जाने के बाद समिति से त्यागपत्र भी दे दिया है।
वैसे देखा जाए तो बकासुर की यह कथा विज्ञान और तकनीक पर न्यौछावर विद्वानों से लेकर अहर्निश भक्तिभाव में डूबे धर्म-प्राणों तक सभी में कमोबेश मौजूद रहती है। सभी को लगता है कि संकट या समस्या का एकमात्र इलाज केवल उनके पास ही मौजूद है। मौजूदा किसान आंदोलन को ही देखें तो जहां सरकार को लगता है कि दो नए कानूनों को रचकर और तीसरे का संशोधन करके उसने सात दशकों की किसानों की समस्याओं को निपटा दिया है, वहीं आंदोलनरत किसान भी इन तीनों सरकारी प्रयासों को खारिज करने से किसानी की व्याधियों से पार पाने का अनुमान लगा रहे हैं। जबकि सचाई यह है कि इन कानूनों को लागू या खारिज करने से किसानी को मुक्ति नहीं मिलने वाली। सरकार ने तीनों कानूनों की मार्फत किसानी को व्यापार में तब्दील करने की जुगत बिठाई है और किसान इन्ही बातों का जबाव देने में लग गए हैं। सरकार और उसे जबाव देने वाले किसानों की ध्यान से सुनें तो लगता है कि किसानी की एकमात्र समस्या बाजार और उससे जुडे भंडारण, परिवहन आदि की ही हैं। जबकि खेती से थोडा-बहुत संबंध रखने वाले भी जानते हैं कि बाजार की पहुंच किसानी के अनेक संकटों में से केवल एक है।
बेहद मामूली स्तर से देखें तो रोजगार के किसी भी प्रयास से अपेक्षा रहती है कि उसकी मार्फत दो वक्त का भोजन मिल पाएगा, जिस साधन से भोजन जुटाया जा रहा है वह दुरुस्त और उत्पादक बना रहेगा और भोजन पैदा करने के श्रम की एवज में उचित मुआवजा या मजदूरी मिल सकेगी। अब इस अपेक्षा को खेती-किसानी से जोडकर देखें तो पता चलता है कि तीनों मामलों में हमारी हालत बदहाल है। दो वक्त के भोजन की सहज प्राप्ति की बजाए दुनिया-जहान के शोध-संस्थान एक देश की तरह हमारी भुखमरी की गुहार लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम चाड, नाइजीरिया सरीखे दक्षिण अफ्रीकी देशों की कतार में बैठे हैं। यही हाल हमारी उपजाऊ मिट्टी और उसकी घटती उत्पादकता का भी है जो खुद सरकारी हिसाब से ही आधी यानि 50 फीसदी बची है। ‘हरित क्रांति’ के पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना जैसे इलाकों में तो मिट्टी की उत्पादकता इतनी कम हो गई है कि यदि रासायनिक खाद का भरपूर ‘डोज’ न दिया जाए तो एक दाना पैदा करना कठिन होगा। इसी तरह की बदहाली उस मुआवजे या मजदूरी की भी है जो किसानों और खेतिहर मजदूरों को उनकी मेहनत के बदले में मिलती है। कडी मेहनत लगाकर पैदा किए गए टमाटर, दूध, सब्जियों सरीखे कृषि उत्पादनों को सडक पर फेंकते किसानों के दृष्य अब हमारे लिए अजूबा नहीं हैं। जाहिर है, यह इसीलिए होता है क्योंकि अपने श्रम और बडी कठिनाई तथा कर्जों के बल पर जुटाई गई दूसरी लागतों के बदले किसानों को न्यायपूर्ण, उचित कीमत और मुआवजा नहीं मिलता।
किसानी संकट के इन बेहद बुनियादी सवालों को हल करने के लिए क्या बकासुर की पद्धति कारगर हो सकेगी? यानि सत्तर साल पहले किन्ही आसमानी-सुलतानी वजहों से अंगीकार की गई कृषि पद्धति आज की किसानी की आपदाओं को बरका सकेगी? यानि लगातार ‘भजा’ जाता ‘उत्पादन और उत्पादकता बढाने’ और ‘बाजार की पहुंच बढाने, आसान करने’ का ‘भजन’ हमारे किसानों को कोई राहत दे सकेगा? यानि ‘बकासुर कथा’ की तरह संकट पैदा करने वालों और उनकी तरकीबों से संकट का निदान पाना कितना कारगर हो सकेगा? यानि कानूनों के अमल या खारिज होने से किसानी की उम्रदराज व्याधियां हल की जा सकेंगी?
दिल्ली की चौहद्दी पर डटे किसानों के आंदोलन ने हमारे इतिहास में एक बेहद कारगर और जरूरी जगह प्राप्त कर ली है। हमारे समाज की गहराई तक व्याप्त जाति, वर्ग, लिंग, रंग आदि के विभाजन इस आंदोलन में पानी भरते दिखाई देते हैं। इस तरह की परिपक्वता, समझ और अहिंसक जज्बे का देशव्यापी अनुभव अभी पिछले साल ‘एनआरसी’ जैसे कानूनों के विरोध में उठे ‘शाहीन बाग’ में दिखाई दिया था। यह जन सैलाव कभी-कभार ही उठता है। ऐसे में जरूरी है कि एक तरफ, सरकार के बनाए कानूनों को खारिज करवाने में अपनी पूरी ताकत लगाई जाए तो दूसरी तरफ, खेती-किसानी की बुनियादी समस्याओं का निदान भी खोजा जाए। सरकार मानती है कि किसानी का संकट उत्पादकता और बाजार तक पहुंच बढाने का संकट है। इसी वजह से सरकार नए कानून भी लाई है। उसके मुताबिक उत्पादकता बढ जाएगी तो कम किसान भी जरूरत भर अनाज का उत्पादन कर सकेंगे। नतीजे में अतिरिक्त श्रम उद्योगों में लगाया जा सकेगा। बेरोजगारी और उत्पादन बढाने की हुलस में जहर-बुझे खाद्यों की पैदावार की तरफ पीठ करके सुझाई जा रही यह तजबीज विश्वबेंक, ‘अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष’ आदि को भी रास आ रही है। वे बार-बार गुहार लगा रहे हैं कि खेती में श्रम यानि किसान को कम किए बिना खेती और उद्योगों का विकास नहीं किया जा सकेगा। जाहिर है, यह तजबीज बकासुर की कथा की तरह ही है। यानि हम संकट पैदा करने वालों से ही उसका हल निकलवाना चाहते हैं। इससे बचना है तो हमें अपनी खेती को लेकर गंभीरता से विचार करना शुरु करना होगा। बकासुर के भरोसे रहे तो सब जानते हैं कि अंत अच्छा नहीं होगा।(सप्रेस)
































