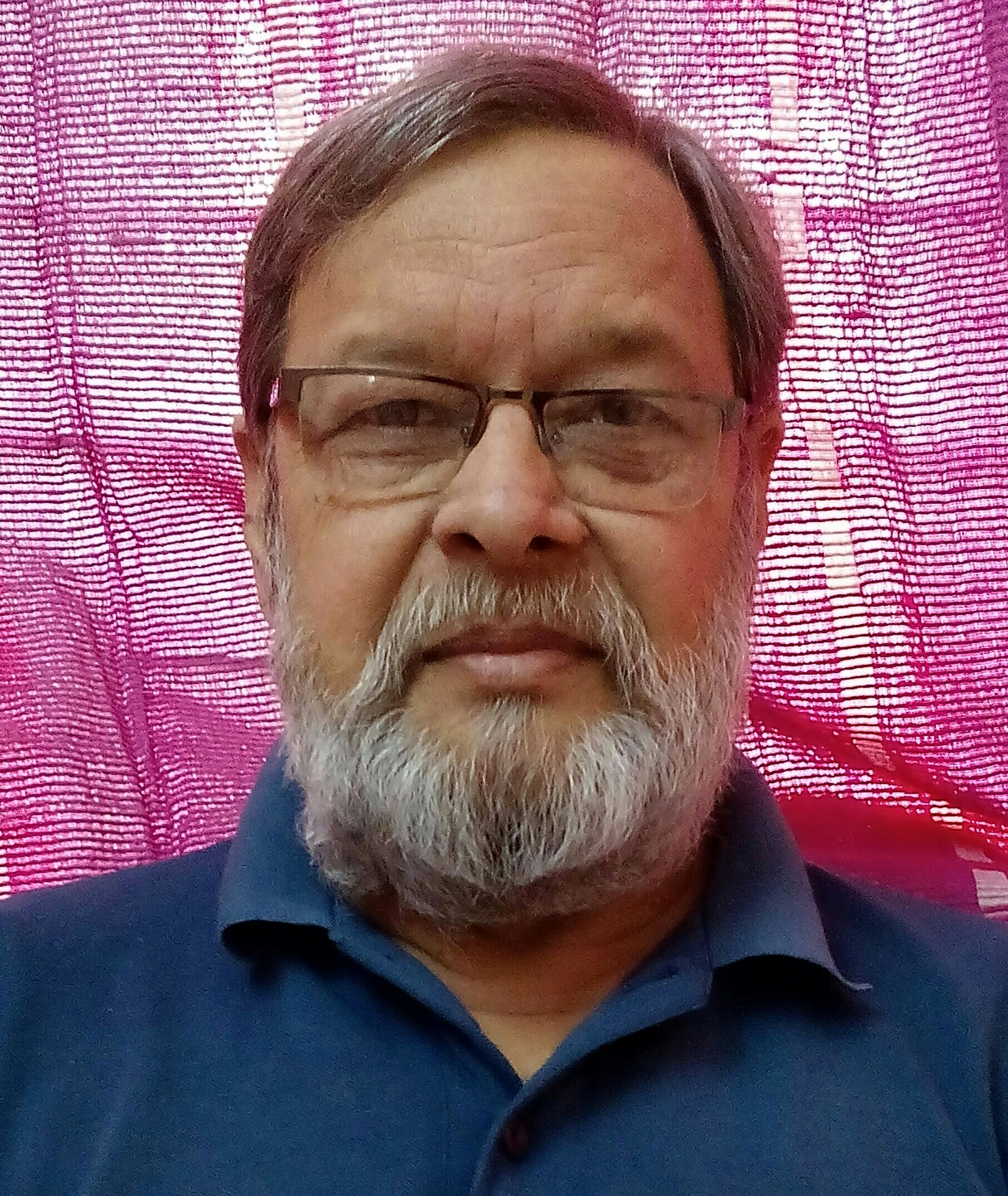
अहिंसक, शांतिपूर्ण और अब तक राजनीतिक दलों से परहेज करने वाले किसान आंदोलन का विकल्प-हीनता की मजबूरी में पनपा यह राजनीति-प्रेम उसे कहां ले जाएगा? कहने को भले ही किसान आंदोलन ‘किसी पार्टी विशेष की वकालत’ न करते हुए भाजपा को हराने की अपील करता दिखाई दे रहा हो, लेकिन व्यवहार में इसका नतीजा किसी-न-किसी पार्टी की जीत होगा। सवाल है कि क्या हमारी प्रातिनिधिक लोकतांत्रिक प्रणाली में केवल चुनावी जीत-हार करती भाजपा समेत सभी राजनीतिक जमातें किसानों की बुनियादी समस्याओं को समझकर उनका हल कर पाएंगी?
आखिर साढ़े तीन महीने से दिल्ली घेरकर बैठे किसान आंदोलन ने सरकार का सामना करने के लिए चुनाव का रास्ता चुन ही लिया। पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों ने किसानों को सत्तारूढ़ राजनीतिक जमातों से टकराने का एक और अवसर उपलब्ध करवाया है। आंदोलन के ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के मतदाताओं से अपील की है कि – ‘भाजपा सरकार तीन किसान विरोधी कानून लेकर आई है जो निर्धन कृषकों एवं उपभोक्ताओं हेतु किसी भी प्रकार के शासकीय संरक्षण को समाप्त कर देते हैं और साथ ही कॉर्पोरेट और बड़े पूंजीपतियों को विस्तार की सुविधा प्रदान करते हैं। उन्होंने किसानों से बिना पूछे किसानों के लिए इस तरह के निर्णय लिए हैं। ये ऐसे कानून हैं जो हमारे भविष्य के साथ-साथ हमारी आने वाली पीढियों को भी नष्ट कर देंगे।’
‘कुछ दिनों में आप सभी राज्य विधानसभाओं के लिए अपने-अपने राज्यों में हो रहे चुनावों में मतदान करेंगे। हम समझ चुके हैं कि मोदी सरकार संवैधानिक मूल्यों, सच्चाई, भलाई, न्याय आदि की भाषा नहीं समझती है। ये लोग वोट, सीट और सत्ता की भाषा समझते हैं। आपमें इनमें सेंध लगाने की शक्ति है।’
‘. . . भाजपा को यह सबक मिलना चाहिए कि भारत के किसानों का विरोध करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। यदि आप उन्हें यह सबक सिखाने में कामयाब होते हैं तो इस पार्टी का अहंकार टूट सकता है और हम वर्तमान किसान आंदोलन की मांगों को सरकार से मनवा सकते हैं।’ ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ का इरादा यह नहीं है कि आपको बताए कि किसे वोट देना है, लेकिन हम आपसे केवल भाजपा को वोट नहीं देने का अनुरोध कर रहे हैं। हम किसी पार्टी विशेष की वकालत नहीं कर रहे हैं। हमारी केवल एक अपील है – कमल के निशान पर गलती से भी वोट न दें।’

आखिर ग्यारह बार की निरर्थक बातचीत, बिजली-पानी बंद करने, रास्तों पर कीलों समेत बाड़ की घेराबंदी करने जैसी तरह-तरह की प्रताड़ना और फूहड़, बेहूदी, अपमानजनक टिप्पणियों के जबाव में किसानों के पास सरकार से निपटने का एकमात्र तरीका चुनाव ही तो बचा है। वैसे भी किसी लोकतांत्रिक, अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलन को महीनों, सालों अनसुना करने वाली सत्ता से राजनीतिक चुनौती ही नतीजे दिलवाती है।
पैंतीस साल के ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’ जैसे अनेक गैर-दलीय आंदोलनों का भी यही अनुभव रहा है। नर्मदा पर बनने और बनाए जाने वाले बड़े बांधों से होने वाले विस्थापन और न्यायपूर्ण पुनर्वास के सवाल पिछली सदी के अंतिम 15 सालों में शिद्दत से उठने लगे थे, लेकिन उन पर किसी ऐसी राजनीतिक पार्टी ने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की जो बदल-बदलकर सत्ता पर काबिज होती रही हैं। वे तब ही कभी-कभार कुछ सक्रिय दिखाई दीं जब उन्हें अपना राजनीतिक नफा-नुकसान दिखाई देने लगा। बांध विरोधी आंदोलन जैसे समूह गैर-दलीय राजनीति करते हैं और उनके लिए चुनाव लगभग अंतिम और मजबूरी का विकल्प हुआ करता है। नतीजे में केवल चुनावी जीत-हार की राजनीति करने और उसी आधार पर सुनने, न-सुनने वाली राजनीतिक पार्टियों ने देश की सर्वाधिक गंभीर समस्याओं में से एक विस्थापन की भी नहीं सुनी।
अहिंसक, शांतिपूर्ण और अब तक राजनीतिक दलों से परहेज करने वाले किसान आंदोलन का विकल्प-हीनता की मजबूरी में पनपा यह राजनीति-प्रेम उसे कहां ले जाएगा? कहने को भले ही किसान आंदोलन ‘किसी पार्टी विशेष की वकालत’ न करते हुए भाजपा को हराने की अपील करता दिखाई दे रहा हो, लेकिन व्यवहार में इसका नतीजा किसी-न-किसी पार्टी की जीत होगा। सवाल है कि क्या हमारी प्रातिनिधिक लोकतांत्रिक प्रणाली में केवल चुनावी जीत-हार करती भाजपा समेत सभी राजनीतिक जमातें किसानों की बुनियादी समस्याओं को समझकर उनका हल कर पाएंगी?
मसलन – सब जानते हैं कि कोविड-19 के कारण भारत समेत समूची दुनिया में पिछला साल बेहद संकट का रहा है। इस संकट का सर्वाधिक खामियाजा किसानों, मजदूरों और गरीबों ने भुगता है। ऐसे में ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना’ (मनरेगा) आडे वक्त में काम आ सकती थी, लेकिन मेघालय को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों में ‘मनरेगा’ की मजदूरी की दर पिछले, यानि 2020-21 के साल से कम, एक रुपया या शून्य रखी गई हैं। आसन्न चुनावों के बावजूद तमिलनाडु, पुडुचेरी में इस साल 17 रुपयों की बढौतरी की गई है, पश्चिम बंगाल में नौ रुपए बढ़े हैं और केरल में कोई वृद्धि नहीं की गई है। ‘मनरेगा’ कानून के मुताबिक मजदूरी की ये दरें ‘उपभोक्ता मूल्य सूचकांक’ और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर केन्द्र सरकार तय करती है, लेकिन दिहाडी की दम पर टिकी गरीब आबादी की मजदूरी बढाने के लिए किसी राज्य सरकार ने आवाज नहीं उठाई। एक तरफ कोरोना के इसी दौर में हर घंटे 90 करोड रुपयों की कमाई करने वाले पूंजीपति हैं और दूसरी तरफ अपनी रोजी-रोटी गंवाने वाले, ‘मनरेगा’ पर निर्भर करीब 11 करोड मजदूर, लेकिन राजनीतिक जमातें इस शर्मनाक अंतर को पाटने के लिए कोई तजबीज नहीं रखतीं। क्या किसान आंदोलन भाजपा को वोट ना देने की अपील करते हुए सत्ता में आने वाली दूसरी पार्टियों की इस या ऐसी ही कमजोरियों का ध्यान रख पा रहा है?
‘आईआईटी-दिल्ली’ में पढ़ा रहीं अर्थशास्त्री रीतिका खेडा के मुताबिक किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों को अब कुछ नए संकटों का सामना करना होगा। मसलन – ताजे आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्ताव रखा गया है कि ‘खाद्य सुरक्षा योजना’ में वितरित किए जाने वाले सस्ते अनाज (मोटा अनाज – एक रुपए, गेहूं – दो रुपए और चावल – तीन रुपए) की कीमतें बढ़ा दी जाएं। दूसरे, इसी ‘खाद्य सुरक्षा कानून’ के तहत लाभ लेने वाली देश की करीब दो तिहाई आबादी की संख्या घटाकर 40 फीसदी कर दी जाए। तीसरे, ‘भारतीय खाद्य निगम’ (एफसीआई) द्वारा गेहूं की खरीद के मापदंडों को और सख्त किया जाए। इस सख्ती में गेहूं की नमी को 14 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करना, मिलावट को 0.75 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत करना जैसी बातें शामिल हैं। सरकार के इन उपायों से किसानों के अलावा जिस आबादी पर भारी असर होगा वह राशन की दुकानों से मिलने वाले अनाज और दूसरी चीजों के बल पर जिन्दा रहती है। रीतिका खेडा कहती हैं कि ‘बेशक देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था मंहगी है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ‘सकल घरेलू उत्पाद’ (जीडीपी) के दो-तीन फीसदी खर्च से एक तरफ गेहूं-धान पैदा करने वाले 15 प्रतिशत किसानों को लाभ पहुंचता है और दूसरी तरफ, सस्ते अनाज के रूप में देश के करीब 66 प्रतिशत लोगों का पेट भरता है।
सवाल है कि क्या देश की राजनीतिक जमातों को इन या ऐसे ही किन्हीं मुद्दों की समझ और उन पर कदम उठाने का हौसला है? और यदि ऐसा नहीं है तो क्या उन्हें यह सब सिखाने की जिम्मेदारी नागरिकों की नहीं होनी चाहिए? पश्चिम बंगाल में 2010-11 में सिंगूर, नंदीग्राम में जमीन के सवालों को लेकर तत्कालीन वाम-मोर्चे की सरकार और कॉर्पोरेट टाटा से आम लोगों ने संघर्ष फांदा था और नतीजे में 37 साल की वाम-मोर्चा सरकार और टाटा कंपनी बाहर हो गए थे। क्या उसी नागरिक पहल से किसान आंदोलन कोई सबक लेना चाहेगा? (सप्रेस)

































