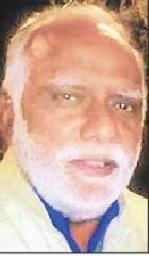
पूंजी की अश्लील बढौतरी के इस जमाने में यह बात बड़े जोर-शोर से कही-उछाली जा रही है कि अब मजदूरों समेत समाज के निचले तबकों की हैसियत समाप्त हो गई है। क्या सचमुच ऐसा है? क्या किसी तरह का, कोई भी विकास बिना मजदूरों की भागीदारी के संभव है? और यदि ऐसा नहीं है तो फिर मौजूदा बदहाली को खुशहाली में तब्दील करने वाले मजदूर लगभग चुप्पी लगाए क्यों बैठे हैं? प्रस्तुत है, ‘अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस’ पर दुनियाभर के मजदूर आंदोलनों की पड़ताल करता बादल सरोज का यह लेख।
1886 की एक मई को शुरू हुयी अमरीकी मजदूरों की राष्ट्रीय हड़ताल के दौरान चार मई को शिकागो के ‘हे मार्केट’ के चौराहे पर काम का समय 8 घंटे किये जाने की मांग को लेकर हुयी मजदूरों की रैली, उसके साथ हुए दमन और साजिशन उनके नेताओं को फांसी चढ़वा देने की घटनाओं ने मजदूरों के अंतर्राष्ट्रीय दिन ‘मजदूर दिवस’ को जन्म दिया था। एक मई दुनिया की ऐसी अकेली तारीख है जो पूरी दुनिया को जोड़ती है, सारे राष्ट्रों और उनकी राष्ट्रीयताओं के ऊपर जाकर उन्हें एक साझी दुनिया के रूप में एकाकार करती है। ‘मई दिवस’ – दुनिया का एकमात्र दिन है जिसे सारी मानवता त्यौहार की तरह मनाती है। इस दिन सभी महाद्वीपों में, दुनिया की हर भाषा, हर बोली में लगभग एक जैसे नारे लगते हैं।
दुनिया भर में ‘मई दिवस’ मनाये जाने की शुरुआत 1889 से हुयी थी। इस तरह महज 133 साल में ‘मई दिवस’ का यह दर्जा हासिल कर लेना मानव इतिहास की अनोखी मिसाल है। कोई भी दिन, विशेषकर मजदूरों से जुड़ा दिन सहज ही इतना लोकप्रिय नहीं होता। सच कितना भी खुल्लमखुल्ला और प्रमाणित क्यों न हो, वह अपने आप लोगों के बीच नहीं पहुंचता। खासतौर से तब, जब सत्ता प्रतिष्ठान के सारे अंग-पुलिस, न्यायपालिका और अखबार पूंजी के चाकरों की तरह काम कर रहे हों। अंतत: वही विचार जिंदा रहते हैं, जिनके लिए लोग मरने को तैयार हों। ‘मई दिवस’ इसी जिन्दा विचार का नाम है।
‘मई दिवस’ संघर्षों के हासिल के लेखे-जोखे का दिन है। इसलिए बजाय इस दिन की महत्ता और ऐतिहासिकता पर ज्यादा विस्तार से चर्चा करने के, आज की दुनिया में मेहनतकशों के संघर्षों की दशा और दिशा पर नजर डाली जाए। हाल के दौर में दुनिया भर के सभी देशों में जितनी अभूतपूर्व जनप्रतिरोध की कार्यवाहियां, हड़तालें हुयी हैं उतनी पिछले कई दशकों में नहीं हुईं। भारत के मेहनतकशों ने इसी 28-29 मार्च को दो दिन की शानदार हड़ताल की, जो नवउदार नीतियों के विरुद्ध हुयी देशव्यापी हड़तालों की श्रंखला में 21वीं थी। पिछली चार हड़तालों में भागीदारों की संख्या, 15, 18, 25 करोड़ से होते हुए इस बार 30 करोड़ तक जा पहुंची। इस तरह के प्रतिरोध के मामले में एशिया में भारत अकेला देश नहीं था; हमारे पड़ोस में बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित जापान और इंडोनेशिया की ट्रेड यूनियनों ने भी इस तरह के आंदोलन किए। फ़्रांस, डेनमार्क, ग्रीस, इटली, पुर्तगाल, स्पेन सहित अन्य यूरोपीय देशों में हड़तालों का लगातार चला सिलसिला आज भी जारी है।

डोनाल्ड ट्रम्प और जो बाइडेन के अमरीका में 1000 से ज्यादा हड़तालें दर्ज की गयीं। पिछले अक्टूबर में तो इतनी हड़तालें हुईं कि उसे ‘स्ट्राइक्टूबर’ ही घोषित कर दिया गया। इन सभी हड़तालों में सिर्फ औद्योगिक मजदूर ही शामिल नहीं थे, उनके साथ नर्स, शिक्षक, डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी, परिवहन कर्मचारी, गैस कर्मचारी, टैक्सी ड्राइवर्स, मॉल के कर्मचारी भी शामिल हुए और पूरे देश को ठप्प करके अपनी शक्ति दिखा दी। डेनमार्क की नर्सों की हड़ताल उनके इतिहास में सबसे लम्बी हड़ताल थी। कुछ ऐसे काम-धंधों में भी हड़तालें हुयीं जिनके बारे में पहले सोचा तक नहीं जाता था, जैसे – ‘अमेज़ॉन’ कंपनी में हड़तालें हुयीं और वे एक देश तक सीमित नहीं रहीं; इटली में हुयी ‘अमेजॉन’ के गोदाम और डिलीवरी के मजदूरों की हड़ताल जल्दी ही जर्मनी, अमरीका और 23 अन्य देशों के ‘अमेज़ॉन सेंटर्स’ पर पहुँच गयी। फ्रांस का ‘येलो वेस्ट आंदोलन’ इसी तरह का एक नया आंदोलन था।
लैटिन अमरीका में अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलम्बिया, इक्वाडोर, उरुग्वे, मैक्सिको आदि में बड़ी हड़तालें हुईं। कोलम्बिया के कोयला मजदूरों की तीन महीने लम्बी हड़ताल ने 6 मजदूरों की मौतें, यौन हिंसा और बर्बरता देखी, मगर वह टूटी नहीं। दक्षिण अफ्रीका सहित अफ्रीकी महाद्वीप के अनेक छोटे-बड़े देशों में हुयी हड़तालों के आयाम भी काफी उल्लेखनीय हैं।
इन संघर्षों की कई विशेषताएं हैं। पिछले तीन दशकों में आमतौर से और 2008 के विश्वव्यापी संकट के बाद से खासतौर से पूँजी और उसके मुनाफे खतरे में पड़े हैं, अस्थिरता बढ़ी है और सरकारों में बिठाये गए दलालों के जरिये इसका सारा बोझ मेहनतकशों पर डाला जा रहा है। यह एक तरफ काम के घंटों में बढ़ोत्तरी, वेतन कटौती, कार्यदशाओं की बदतरी का रास्ता अपना रही है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल सहित सार्वजनिक खर्चों में कटौती और उनके निजीकरण के जरिये जीवन का खर्च बढ़ाया जा रहा है।
इस सबके खिलाफ आक्रोश का विस्फोटक होते जाना इस कालखण्ड की एक विशेषता है। इसकी दूसरी खासियत है – मजदूर आंदोलन द्वारा जनता के बाकी हिस्सों; किसानों – छात्रों – महिलाओं की मांगें उठाना। इसका असर यह हुआ है कि ये तबके भी मजदूर आंदोलन का हिस्सा बने हैं। मजदूरों की हड़तालें आम हड़तालों का रूप ले रही हैं। इनका राजनीतिक असर भी हुआ है; कई देशों, लैटिन अमरीका ही नहीं स्कैंडिनेवियन देशों में भी सरकारें बदली हैं। अमरीका तक में घोषित समाजवादी वहां की कांग्रेस, सीनेट और राज्यों की ‘प्रतिनिधि सभाओं’ में जीतकर पहुंचे हैं।
हाल के संघर्षों की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि मेहनतकश न केवल अपने तात्कालिक मुद्दों को उठा रहे हैं, बल्कि उन नीतियों के विरुद्ध भी लड़ रहे हैं जिनकी वजह से ये तात्कालिक समस्याएं उपजती हैं। इस तरह वे सिर्फ परिणाम से ही नहीं, कारण से भी लड़ रहे हैं और अनजाने ही श्रमिक आंदोलन की उस बदनाम व्याधि से उबरने की कोशिश कर रहे हैं जिसे “अर्थवाद” कहा जाता है। यह शुभ लक्षण है। उदाहरण के लिए भारत के किसान आंदोलन ने चार लेबर कोड्स का सवाल अपनी मांगों में जोड़ा तो देश की ट्रेड यूनियनों के साझे मंच ने तीन कृषि कानूनों की वापसी की मांग दोहराई। दुनिया के अनेक देशों के श्रमिक आंदोलनों ने पूँजी की लूट से होने वाली पर्यावरणीय हानि का सवाल भी अपनी सक्रियता के मुद्दों में शामिल किया है।
इन संघर्षों का मूल्यांकन करते समय एक बात याद रखना जरूरी है। पिछली शताब्दी की आख़िरी दहाई में दुनिया में समाजवादी व्यवस्था को लगे आघात और उसके बाद विश्व के एकध्रुवीय हो जाने ने सभी देशों की, तब तक की, अर्थव्यवस्थाओं पर विश्वबैंक, आईएमएफ, डब्लूटीओ का त्रिशूल ही नहीं घोंपा था; एक मनोवैज्ञानिक असर भी डाला था। फ्रांसिस फुकोयामा के “इतिहास के अंत” की, अब खुद उनके द्वारा ठुकराई गयी थीसिस के अनुरूप गढ़े गए आख्यान की मीडिया, साहित्य, फिल्म, पाठ्यक्रमों आदि के माध्यम से ‘बमबारी’ की गयी। पूँजीवाद की चिरन्तरता के भरम की बौछारें की गयीं।
ऐसा नहीं कि इनका असर नहीं हुआ। लोगों के सोचने, समझने और गतिशील होने में यह दिखा। यह हमला सिर्फ आर्थिक शोषण और पूँजी के वर्चस्व को निर्द्वन्द तरीके से स्थापित करने भर का नहीं था। इस हमले का एक वैचारिक आयाम भी था। इसने अपनी लूट को पूरी निर्लज्जता के साथ अंजाम देने के पहले जनता पर अपना वैचारिक वर्चस्व कायम किया था। यह दो रूपों में दिखता था/है। एक तो यह कि इसने ‘टीना’ (‘देयर इज नो ऑल्टरनेटिव,’ अब कोई विकल्प नहीं) फैक्टर को लगभग नियति बनाकर रख दिया। इसका विस्तार लोगों की इस मानसिकता में दिखा कि; “अब कुछ नहीं हो सकता, अब आंदोलन – संघर्ष वगैरा करने का कोई लाभ नहीं है।” चूंकि ये नीतियां दुनिया भर में अमल में लाई जा रही थीं/हैं इसलिए यह प्रभाव भी विश्वव्यापी था। हाल के विश्वव्यापी आंदोलनों ने काफी हद तक इसे खंडित किया है।
बहरहाल, इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ‘हरा-हरा’ ही है। साम्राज्यवादी पूँजी इतनी आसानी से हार स्वीकार नहीं करती। वे जब ऊपर से किये गए दमन से कुचलने में नाकाम होते हैं तो नीचे से विभाजन और विघटन पैदा करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी, कट्टरतावादी, फूटपरस्त ताकतों का उभार और उनका सत्ता में पहुंचना अनायास नहीं है। यह उस ‘ग्रैंड प्लान’ का हिस्सा है जिसे सैमुएल हटिंग्टन नामक कथित बुद्धिजीवी ने “सभ्यताओं के टकराव” का नाम दिया था। बढ़ती भागीदारियों, समावेशी होती मांगों से लगता है कि अब यह जड़ता टूट रही है। बात निकली है तो जाहिर है, यहीं तक नहीं रुकेगी – दूर तलक जाएगी। 2022 का ‘मजदूर दिवस’ दुनिया के मेहनतकशों के लिए उपलब्धि, विस्तार और उसी के साथ चुनौतियों का ‘मई दिवस’ है। (सप्रेस)

































