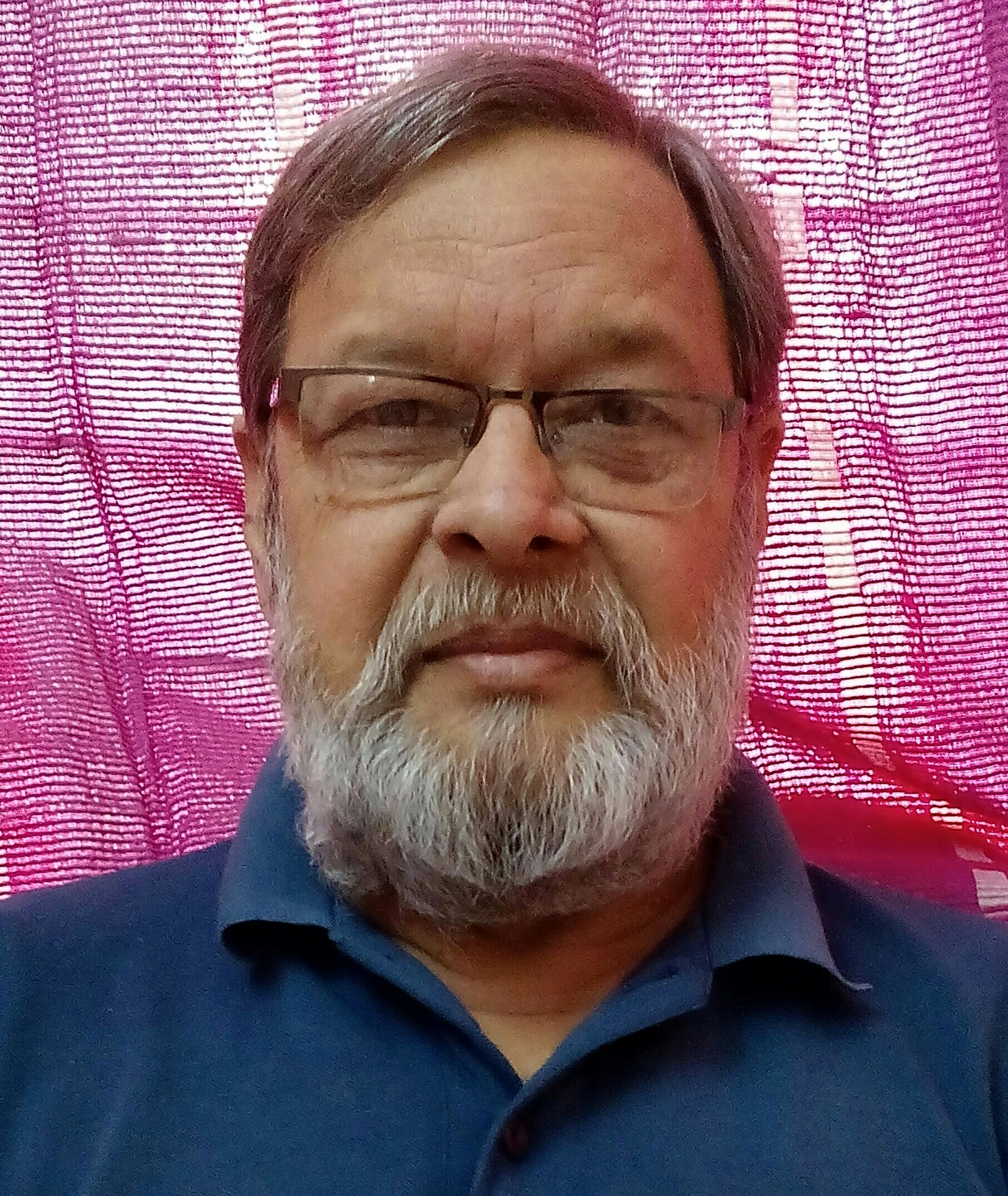
जिस लोकतंत्र की कसमें खाकर हम अपने तमाम अच्छे-बुरे, निजी-सार्वजनिक काम निकालते रहते हैं और किसी दूसरी राजनीतिक जमात के सत्ता पर सवारी गांठने से जिस लोकतंत्र की हत्या होना मान लिया जाता है, ठीक उसी लोकतंत्र की एन नाक के नीचे अभी कुछ महीने पहले करोडों मजदूर अपने-अपने गांव-देहात लौटे हैं। कहा तो यह जा रहा है कि कोरोना वायरस से उपजी कोविड-19 बीमारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में रोजगार के ठप्प होने से करोडों मजदूर वापस अपने-अपने गांवों की ओर कूच कर गए थे, लेकिन क्या इस विशाल ‘घर-वापसी’ की वजह मात्र इतनी ही है? और अगर इसे मान भी लिया जाए तो इससे निपटने के लिए लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं ने आखिर क्या किया? क्या विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पलायन और प्रति-पलायन करते इन मजदूरों के प्रति अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभा पाईं?
कोरोना-काल के अपने छठवें संबोधन में प्रधानमंत्री ने जिन दो विशेष बातों को प्रमुखता से रखा है उनमें से एक, ‘सिविल सोसायटी’ की भूमिका की मंजूरी है। ‘सिविल सोसायटी’ ऐसा कमाल का संबोधन है कि देशभर में यत्र-तत्र बिखरे एनजीओ से लगाकर तरह-तरह के नागरिक समूह प्रधानमंत्री के उसके उल्लेख भर कर देने से बल्ले-बल्ले कर रहे हैं। उनमें से इक्का–दुक्का आत्ममुग्ध एनजीओ तो यहां तक कहने लगे हैं कि भूख से निपटने की प्रधानमंत्री की योजना दरअसल उनने पहले ही बता दी थी। प्रधानमंत्री की दूसरी घोषणा आधी से अधिक आबादी के लिए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ की मार्फत 80 करोड लोगों के लिए भोजन के इंतजाम से जुडी है। इस योजना में हरेक को हर महीने पाँच किलो गेहूं या चावल और एक किलो दाल दी जाएगी। पहले इसे लॉकडाउन के प्रभाव में घर वापस लौटे गरीब मजदूरों की भूख और लबालब भरे अन्न-भंडारों से जोडकर क्रियान्वित करने की मांग की जा रही थी, अब बिहार चुनावों के मद्देजनर खुद प्रधानमंत्री ने इसे नवम्बर तक बढाकर घोषित कर दिया है। जिस योजना के लाभार्थी ढाई-गुने अमरीका, बारह गुने ब्रिटेन और दो-गुने यूरोपियन यूनियन’ की टक्कर के हों तो उसकी तारीफ ही की जानी चाहिए।
आज से करीब 19 साल पहले, जब केन्द्र में ‘संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन’ यानि ‘यूपीए’ की पहली पारी की सरकार थी, यही सवाल पहली बार उठा था। उन दिनों देश में जगह-जगह से आने वाले भुखमरी के समाचारों के अलावा अनाज के विपुल उत्पादन और उसके खुले में सडने की खबरें भी आया करती थीं। एक तरफ, भारी मात्रा में उत्पादन और दूसरी तरफ, भंडारण के अभाव में अनाज की बर्बादी से निपटने पर सुझाव देने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किेया गया था। इस समिति ने अतिरिक्त सडते अनाज को समुद्र में फेंकने तक की अनुशंसाएं की थीं। भुखमरी और सडते अनाज के विरोधाभास को लेकर देशभर से आवाजें उठने लगी थीं और मांग की जा रही थी कि इस अतिरिक्त अनाज को भूखों में बिना-मूल्य वितरित कर दिया जाए। बार-बार कहने के बावजूद केन्द्र के अनसुना करने पर मानवाधिकार समूह ‘लोक स्वातंत्र्य संगठन’ यानि ‘पीयूसीएल’ ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका लगाई थी। वर्ष 2001 में लगाई गई इस ख्यात याचिका पर अदालत ने भी अतिरिक्त अनाज के भंडारण की व्यवस्था करने और आम भूखे लोगों में मुफ्त वितरित करने की अनुशंसा की थी। किसान की मेहनत और भूखों के पेट के बीच अदालत द्वारा सुझाई गई इस सीधी कडी पर केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने यह कहकर अडंगा लगा दिया था कि इससे किसानों की आय पर विपरीत प्रभाव पडेगा। हालांकि दबे-छिपे कहा तो यह भी गया था कि पवार साब शराब निर्माताओं के लिए अनाज सडा रहे हैं।
अब, करीब दो दशक बाद प्रधानमंत्री की पहल पर अनाज के मुफ्त वितरण को लेकर कृषि-नीति विश्लेषक देवेन्दर शर्मा तक संतुष्ट हैं। शर्मा का कहना है कि ‘एक तरफ अनाज का भरपूर भंडार है और दूसरी तरफ करोडों लोग भूखे हैं। ऐसे में यह कदम सराहनीय है।‘ सरकारी हलकों के हवाले से कहा जा रहा है कि आज की तारीख में हमारे भंडारों में इतना अनाज है, जिससे करीब चार साल तक बिना कुछ किए देशभर की आबादी को खिलाया जा सकता है। यानि भूखों के लिए हमारे पास पर्याप्त से अधिक अनाज उपलब्ध है। सवाल है कि भूखे कितने हैं? ‘भारतीय खाद्य निगम’ के भंडारण का अध्ययन करने की खातिर बनाई गई ‘शांताकुमार समिति’ की नजर से देखें तो पता चल सकता है कि लबालब भरे भंडारों का अनाज कुल छह फीसदी किसानों से सरकारी खरीद के जरिए उगाया गया अनाज है। यानि मंडियों तक न पहुंच पाने वाले करीब 94 प्रतिशत किसान अपने-अपने कृषि उत्पादनों को स्थानीय स्तर पर औने-पौने दाम में ठिकाने लगा रहे हैं। अलबत्ता, इतना तो साफ है कि इन्हें अपने पेट भरने के लिए किसी तरह की सहायता की जरूरत नहीं होगी।
पिछले दो महीनों से दो आंकडे खासतौर पर उछल रहे हैं। एक, देश की कुल कामकाजी आबादी में से 92-94 फीसदी अनौपचारिक, असंगठित क्षेत्र का है। दूसरे, पलायन करने और लौटने वाले मजदूरों की कुल संख्या 40 करोड के आसपास है। यानि देश की लगभग एक तिहाई आबादी काम की आस और दाल-रोटी की आशा में दर-दर की ठोकरें खाती फिरती है। खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जाने वाली जिस 80 करोड आबादी का प्रधानमंत्री अपने भाषण में जिक्र करते हैं वह इस 40 करोड को मिलाकर बनी है। जाहिर है, जिन्हें हम सर्वहारा, सर्वाधिक गरीब मानते हैं उनका पेट आसानी से भरा जा सकता है। तो फिर व्यापक पैमाने पर, हर कहीं दिखती भुखमरी की वजह क्या है? आखिर इतनी बडी संख्या में लोगों को क्यों अपना घर-बार छोडकर मारे-मारे फिरना पडता है? क्या इनकी घर छोडने की मजबूरी के प्रति, बाद में भोजन बांटकर वाह-वाही लूटने वाली नाना प्रकार की लोकतांत्रिक संस्थाओं का कोई दायित्व नहीं बनता? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उनकी छत्र-छाया में पलने वाली गैर-सरकारी संस्थाएं ऐसी कौन-सी पद्धति का विकास करती हैं जिसके अंत में भरपूर अनाज के बावजूद करोडों लोग भूखे मर जाते हैं या फिर रोजगार की खातिर दर-दर भटकते हैं?
जिस लोकतंत्र की कसमें खाकर हम अपने तमाम अच्छे-बुरे, निजी-सार्वजनिक काम निकालते रहते हैं और किसी दूसरी राजनीतिक जमात के सत्ता पर सवारी गांठने से जिस लोकतंत्र की हत्या होना मान लिया जाता है, ठीक उसी लोकतंत्र की एन नाक के नीचे अभी कुछ महीने पहले करोडों मजदूर अपने-अपने गांव-देहात लौटे हैं। कहा तो यह जा रहा है कि कोरोना वायरस से उपजी कोविड-19 बीमारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में रोजगार के ठप्प होने से करोडों मजदूर वापस अपने-अपने गांवों की ओर कूच कर गए थे, लेकिन क्या इस विशाल ‘घर-वापसी’ की वजह मात्र इतनी ही है? और अगर इसे मान भी लिया जाए तो इससे निपटने के लिए लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं ने आखिर क्या किया? क्या विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पलायन और प्रति-पलायन करते इन मजदूरों के प्रति अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभा पाईं? पिछले तीन-साढे तीन महीनों के अनुभवों को ही देख लें तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज को आसानी से परखा जा सकता है। मसलन – सब जानते थे कि रोजगार के ठप्प हो जाने के बाद मजदूर अपने-अपने गृह-ग्राम ही वापस लौटेंगे। शहरों, औद्योगिक बस्तियों में इतनी मुरव्वत और क्षमता तो नहीं होती कि किसी को कुछ महीनों बिना काम अपने यहां टिकाए रख सके। तो जब सब जानते थे कि मजदूरों को हजार-हजार किलोमीटर और कहीं-कहीं तो समूचा देश पार करके अपने-अपने घर पहुंचना है तो पहले से वैसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गईं? पैदल लौटते मजदूरों को क्यों सीमित संसाधनों, छोटे कामकाजी ढांचों और बेहद स्थानीय समझ वाली ‘सिविल सोसाइटी’ के हवाले कर दिया गया? ये और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं असफल साबित हुई हैं। जाहिर है, ऐसे में हमें उनके कामकाज, बुनियाद और भारतीय संदर्भ में प्रासंगिकता को गहराई से देखना होगा। क्या हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं मौजूदा विकास की ठीक, उपयुक्त और कारगर समझ बना पा रही हैं?
































