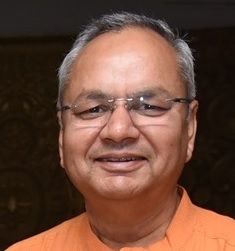
हाल के दिनों में देशभर में साम्प्रदायिकता का जहर तेजी से फैला है और नतीजे में समाज का तीखा विभाजन हो रहा है। ऐसे में महात्मा गांधी ही याद आते हैं। वे होते तो ऐसे हालातों में आखिर क्या करते? क्या होती, उनकी सीखें?
भारत, जिसे विविधता में एकता का प्रतीक माना जाता है, आज एक बार फिर साम्प्रदायिक तनाव की आग में झुलस रहा है। हाल के महीनों में संभल (उत्तरप्रदेश), महू (मध्यप्रदेश) और नागपुर (महाराष्ट्र) जैसे क्षेत्रों में हुए दंगे न केवल सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर रहे हैं, बल्कि देश की समरसता और सहिष्णुता की पहचान को भी गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। ये घटनाएं समाज में शांति और सौहार्द के लिए चुनौती बन गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप हिंदू-मुस्लिम, सिख-ईसाई और अब जैन व बौद्ध समुदायों के बीच अविश्वास की खाई चौड़ी हो रही है।
बहुसंख्यक वर्ग के निशाने पर अल्पसंख्यकों का आना चिंता का विषय है। इन दंगों का प्रभाव केवल सामाजिक ताने-बाने तक ही सीमित नहीं है—व्यापार और उद्योग ठप्प होने से आर्थिक नुकसान हो रहा है, सार्वजनिक व निजी सम्पत्ति नष्ट हो रही है, निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और नफरत का यह चक्र तेजी से फैल रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की सहिष्णु छवि पर सवाल उठ रहे हैं, जो देश की साख के लिए खतरा है।
संभल से नागपुर तक हिंसा की जड़ें तेजी से फ़ैली हैं। संभल में तनाव तब भड़का जब स्थानीय अदालत ने जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया। दावा था कि मुगल बादशाह बाबर ने इसे एक मंदिर को तोड़कर बनवाया था। सर्वेक्षण के दौरान हिंसा ने विकराल रूप ले लिया—लोग मारे गए, संपत्ति नष्ट हुई, और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। दूसरी ओर, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों ने भावनाएं भड़काईं। इसी बीच, समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को “क्रूर नहीं, बल्कि कुशल प्रशासक” बताकर विवाद को हवा दी। इसके जवाब में महाराष्ट्र विधानसभा ने उन्हें “देशद्रोही” करार देते हुए निलंबित कर दिया। नागपुर में ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ (आरएसएस) के मुख्यालय के निकट हुई हिंसा ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह हिंसक घटना ‘घर में घुसकर मारने की प्रवृत्ति’ का एक नया परिचायक है?! ये घटनाएं दर्शाती हैं कि ऐतिहासिक विवाद और धार्मिक पहचान से जुड़े मुद्दे आज भी समाज को बांटने की ताकत रखते हैं।

राजनीति और साम्प्रदायिकता का चोली-दामन का साथ रहा है। हमें यह याद रखना चाहिए कि ‘मुस्लिम लीग’ की मुस्लिम-परस्त राजनीति और ‘हिन्दू महासभा’ के ‘पितृ-भूमि’ और ‘पुण्य-भूमि’ के विचार ने आग में घी डालने का काम किया था और अतंत: देश के विभाजन का कारण बना था। आजकल हो रही राजनीतिक बयानबाजी इस आग को एक बार फिर भड़का रही है। चुनावी मौसम में ‘80 बनाम 20 फीसद,’ ‘अब्बा जान के पास राशन,’ ‘मस्जिदों में अवैध गतिविधियां’ और ‘बुलडोजर नीति’ जैसे बयान ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं।
हिंदुत्व के समर्थक नेता महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी से लेकर बाबर व औरंगजेब तक के मध्ययुगीन शासकों को निशाना बनाते हुए गंगा-जमुनी तहजीब की आलोचना करते हैं, तो विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ उकसावा करार देता है। भाजपा इसे तुष्टिकरण के खिलाफ अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा का हिस्सा बताती है। दुर्भाग्यवश, चुनाव आयोग का रिकार्ड भी इस मामले में निष्पक्ष नहीं दिखता है। उसने ऐसे भड़काऊ बयानों पर ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे नेताओं, विशेषकर सत्तारूढ़ दल को खुली छूट मिलती रही। संसद तक में साम्प्रदायिक टिप्पणियां आम हो गई हैं। सबसे चिंताजनक है कि नौकरशाही और पुलिस, जो कभी धर्मनिरपेक्षता की मिसाल थीं, अब पक्षपात और साम्प्रदायिक बयानों में लिप्त दिख रही हैं और इसे सत्ताधारी नेताओं का समर्थन प्राप्त है।
गांधीजी की दूरदर्शिता ने, जिसका हिन्दुत्ववादी संगठन 1920 से ही विरोध करते रहे हैं, साम्प्रदायिकता के इस जहर को उसी वक्त पहचान लिया था और हिन्दू-मुस्लिम एकता को देश की आज़ादी व विकास के लिए आवश्यक बताया था। महात्मा गांधी ने ‘यंग इंडिया’ (29 मई 1924) में एक लेख लिखकर हिंदू-मुस्लिम एकता को सबसे बड़ी चुनौती माना था। उन्होंने इसके कारणों, जैसे – अरबों के वंशजों की लड़ाका प्रवृत्ति, मोपला समुदाय की हिन्दुओं के खिलाफ बर्बर हिंसा, आर्य समाज द्वारा चलाये जा रहे शुद्धि आंदोलन, मुसलमानों की गौवध की जिद और हिन्दुओं द्वारा मस्जिदों के सामने बाजे-गाजे के साथ जुलूस निकालने का गहरा विश्लेषण किया था।
गांधीजी ने सदैव मुस्लिमों की आक्रामकता और हिन्दुओं की कायरता तथा दब्बूपन की आलोचना की। गांधीजी ने “यंग इंडिया” के अगले अंक में लिखा कि ‘इन दोनों मजहबों को मानने वाले लोग अपना फ़र्ज़ किस तरह अदा करते हैं इसी आधार पर भावी पीढ़ियां इनके बारे में अपना निर्णय देंगी। हिन्दू धर्म और इस्लाम धर्म के उसूल चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हों, दोनों की खूबियों और खामियों का निर्णय सिर्फ इसी बात से किया जा सकता है कि ये समष्टि रूप में अपने अनुयाइयों पर कैसा असर डालती हैंI’

गांधीजी का उपरोक्त विश्लेषण आज भी प्रासंगिक हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इस समस्या में और भी नए कारक जुड़ गए हैं – वोट बैंक की राजनीति, सोशल-मीडिया पर अफवाहें, ऐतिहासिक घटनाओं की गलत व्याख्या, आर्थिक असमानता से ध्यान हटाने की कोशिश, प्रशासन की निष्क्रियता और अदालती देरी भी हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। ‘टीआरपी’ बढाने के चक्कर में इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया की बेसिरपैर की निरर्थक बहसें अक्सर साम्प्रदायिक तनाव को बढाने में मदद करती हैं। नागपुर की घटना ने गांधीजी के विचारों की प्रासंगिकता को फिर से रेखांकित किया है।
आखिर इस जहर के समाधान का रास्ता कहाँ से निकलेगा? हम गांधी से प्रेरणा लेकर उनके द्वारा बताये गए अहिंसा, सत्याग्रह और ‘सर्व-धर्म, सम-भाव’ के जरिए शांति के मार्ग पर चल सकते हैं। आज जरूरत है : शिक्षा और जागरूकता के द्वारा न केवल बच्चों को बचपन से, वरन युवाओं और बुजुर्गों को भी धार्मिक सहिष्णुता का प्रशिक्षण दिया जाय। विभिन्न समुदायों के नेताओं के बीच बातचीत का सतत सिलसिला शुरू किया जाए जिससे गलतफहमियां दूर हों। प्रशासन और पुलिस निष्पक्ष होकर काम करे तथा कानून का सख्त और निष्पक्ष पालन हो।
भारत की सांस्कृतिक एकता को बढाने धार्मिक मेलों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिससे आपसी सौहार्द बढ़े। अफवाहों पर लगाम लगाने, सोशल-मीडिया पर झूठ को रोकने के लिए सरकार और जनता साथ आएं एवं इस हेतु ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ (एआई) का उपयोग सूचना की सत्यता जांचने में किया जा सकता है। समुदाय विशेष के आर्थिक बहिष्कार की घोषणा करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ऐतिहासिक विषयों पर निर्मित फिल्मों की समीक्षा सेंसर-बोर्ड के अलावा अकादमिक इतिहासकारों से भी करवाई जाए।
साम्प्रदायिक दंगे समाज के लिए जहर हैं। गांधीजी का संदेश—अहिंसा, प्रेम और सहिष्णुता आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो भारत को इस संकट से उबारा जा सकता है। यह समय एकजुट होने का है, न कि बंटवारे का। क्या हम गांधीजी के सपनों का भारत बना पाएंगे? यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। (सप्रेस)

































