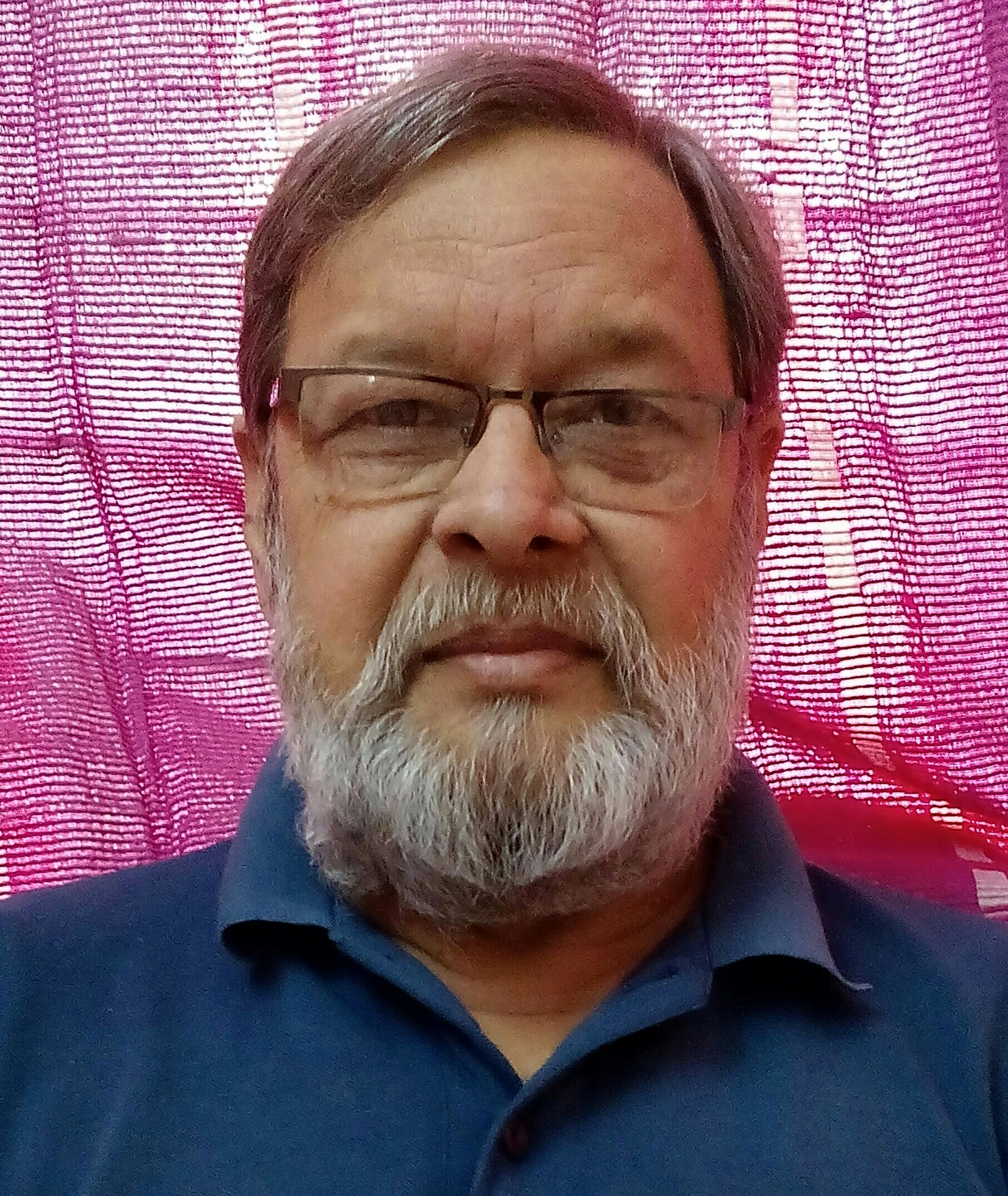
तमाम अटकल-पच्चियों के बावजूद सवाल है कि क्या हमारा समाज आजादी के बाद के सबसे बडे पलायन को भोगने की तकलीफों को महसूस करना भी छोड़ चुका है? या फिर ‘पहचान,’ ‘धर्म’,’ ‘बहु-संख्यकवाद’ जैसी कोई और बात है जिसके चलते आम लोग अपने दुख-दर्द भुला देते हैं? या फिर अध्ययन-कर्ताओं समेत विस्तारित मध्य और उच्च-मध्य वर्ग अपने ही समाज के ‘निचले’ तबकों के बारे में निरा अनजान है?
‘राहत’ इंदौरी की विदाई ने साहित्यिक हलकों में एक बार फिर वही पुराना ‘लोकप्रिय बनाम शास्त्रीय’ का मुद्दा छेड़ दिया गया है। ‘राहत’ भाई की धुआंधार लोकप्रियता में डूबते-उतराते कई लोग उन्हें आवाम की आवाज कह रहे हैं तो कुछ विद्वान उन पर ‘लोकप्रिय’ होने की तोहमत लगा रहे हैं, गोया लोकप्रिय होना शास्त्रीय अर्थों में साहित्यकार होना नहीं माना जा सकता। गजल गायक जगजीत सिंह के शुरुआती दौर में उन पर भी यह आरोप थे कि उन्होंने गजल को लोकप्रियता के नाम पर ‘हलका’ कर दिया है। कई विद्वान साहित्यकार आज भी मानते हैं कि पचास-बावन साल और दर्जनों संस्करणों वाली ‘रागदरबारी’ केवल मनोरंजन की किताब है और उसमें सम-सामयिक समाज का कोई भरोसेमंद विश्लेषण नहीं है। कुल मिलाकर घूम-फिरकर सवाल यही है कि क्या लोकप्रियता शास्त्रीयता से कमतर और अल्प-जीवी होती है और लाखों-लाख लोगों को प्रभावित करने वाली रचना असल में साहित्य या कलाओं के संसार में दो-कौडी की हैसियत नहीं रखती?
भोपाल में तब के ‘शासन साहित्य परिषद’ की कार्यक्रम श्रंखला ‘समय और हम’ में बोलते हुए हरिशंकर परसाई ने एक मार्के की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि साहित्य सृजन का ‘कच्चा माल’ समाज ही देता है, जिसे बाद में अपने विचार, शैली, भाषा और अनुभवों के जरिए सजा-संवारकर साहित्यकार वापस उसी समाज के सामने पेश कर देता है। कुम्हार, मिट्टी और मटके के आपसी रिश्तों का उदाहरण देते हुए परसाई जी ने इसे रचना प्रक्रिया की द्वंद्वात्मकता बताया था। सवाल है कि किसी विधा की रचना प्रक्रिया में समाज नाम के ‘कच्चे माल’ का आजकल कितना हिस्सा होता है? क्या हमारा साहित्य और दूसरी कलाएं समाज, खासकर निम्न और निम्न-मध्यवर्गीय समाज की धडकन पहचान पाती हैं? क्या रचनाकार उस समाज को ठीक जानता-पहचानता है जिसके बारे में उसकी रचनाएं अहर्निश गुहार लगाती रहती हैं? और सबसे अहम, क्या रचनाकार समाज नाम की ‘कच्ची मिट्टी’ से अपनी भौतिक, संवेदनात्मक और आध्यात्मिक दूरी को पहचान पा रहा है?
साहित्य और कलाओं के ही रिश्तेदार मीडिया की ‘कच्ची मिट्टी’ यानि जीते-जागते समाज से कोसों दूरी की बानगी पिछले अनेक चुनावों में की गई उसकी उन भविष्यवाणियों से बुरी तरह उजागर हो गई थीं जिनमें इस-या-उस राजनीतिक जमात को विजयी या हारता हुआ बताया जा रहा था और नतीजे भविष्यवाणियों के ठीक विपरीत आ रहे थे। देसी मीडिया में कृषि और ग्रामीण जीवन की लगातार घटती हैसियत और उनकी ‘बीट’ समाप्त होने को इसकी वजह बताया गया था, लेकिन फिर ‘न्यूयार्क टाइम्स’ को क्या हो गया था जिसने एन चुनाव के नतीजों के एक दिन पहले हिलरी क्लिंटन की जीत बताते हुए पूरे पहले पन्ने पर उनका फोटू छापा था। सब जानते हैं, एक दिन पहले की गई इस ‘पक्की’ भविष्यवाणी के ठीक विपरीत चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रम्प की जीत हुई थी। जाहिर है, देशी हो या विदेशी, मीडिया अपनी-अपनी ‘कच्ची मिट्टी’ को पढ़ने, पहचान पाने में नकारा साबित हुआ है।
कला-साहित्य–मीडिया की तरह यदि हम अपने आसपास की राजनीति को भी देखें तो ‘कच्ची मिट्टी’ से दूरी का यह कारनामा वहां ज्यादा तीखे रूप में दिखाई देता है। अभी पिछले हफ्ते न्यूज-पोर्टल ‘गांव कनेक्शन’ और ख्यात शोध संस्थान ‘सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डॅवलपिंग सोसाइटीज’ (सीएसडीएस) के लॉकडाउन के दौरान हुए अनुभवों पर एक रिपोर्ट आई है। मई 30 से जुलाई 16 के बीच देश के 20 राज्यों, जिनमें दक्षिण के चार बडे राज्य शामिल नहीं हैं, और तीन केन्द्र शासित क्षेत्रों के 179 जिलों में 25 हजार लोगों के रूबरू साक्षात्कार के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट में बताया गया है कि तरह-तरह के संकटों, चिंताओं और कमियों के बावजूद लोगों को मौजूदा केन्द्र और राज्य सरकारों पर पूरा भरोसा है। रिपोर्ट में 78 फीसदी लोगों ने कहा है कि उनके यहां काम पूरी तरह ठप्प है, 68 फीसदी लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और 77 फीसदी के गांवों में रोजगार की समस्या है। पांच फीसदी परिवारों को छोडकर बाकी सभी पर लॉकडाउन का असर पड़ा है, एक तिहाई परिवारों को लॉकडाउन के दौरान बहुत बार (12 फीसदी) और कई बार (23 फीसदी) पूरा दिन भूखा रहना पड़ा है। उन्हें घर खर्च के लिए कर्ज लेना पड़ा है और जायदाद, जेवर, जमीन आदि बेचना पडे हैं। दो तिहाई प्रवासी मजदूरों ने बताया कि उन्हें सरकारी खाना नहीं मिला और आठ में से एक प्रवासी मजदूर की पुलिस ने पिटाई भी की।
विडंबना यह है कि इन तमाम-ओ-तमाम दुख, तकलीफों के बावजूद, इसी अध्ययन के मुताबिक 74 फीसदी लोग केन्द्र और राज्य सरकारों के कदमों से संतुष्ट पाए गए। यहां तक कि प्रवासी मजदूरों के दो-तिहाई हिस्से ने भी सरकारी कार्रवाइयों से संतुष्टि जाहिर की। लॉकडाउन के संकटों पर कमोबेश इसी तरह का अध्ययन मीडिया समूह ‘इंडिया टुडे’ ने भी करवाया था और उसके नतीजे भी लगभग ऐसे ही थे। यानि ढेर सारी असहनीय पीड़ाओं के बावजूद समाज में अपनी सरकारों से कोई गिला-शिकवा नहीं पाया गया। मानो तकलीफें और सरकार दो अलग-अलग बातें हैं और उन्हें चुनने या भोगने के मापदंड भी भिन्न-भिन्न। तमाम अटकल-पच्चियों के बावजूद सवाल है कि क्या हमारा समाज आजादी के बाद के सबसे बडे पलायन को भोगने की तकलीफों को महसूस करना भी छोड़ चुका है? या फिर ‘पहचान,’ ‘धर्म’,’ ‘बहु-संख्यकवाद’ जैसी कोई और बात है जिसके चलते आम लोग अपने दुख-दर्द भुला देते हैं? या फिर अध्ययन-कर्ताओं समेत विस्तारित मध्य और उच्च-मध्य वर्ग अपने ही समाज के ‘निचले’ तबकों के बारे में निरा अनजान है?
अर्थशास्त्री प्रोफेसर रामप्रताप गुप्ता ने मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह और उत्तरप्रदेश में मायावती की सरकारों के अपने तुलनात्मक अध्ययन में बताया था कि तरह-तरह की आर्थिक योजनाओं, नीतियों के बावजूद दिग्विजय सिंह दलित वोटों को अपनी तरफ नहीं खींच पाए थे। दूसरी तरफ, पहचान और अस्मिता की राजनीति करने वाली मायावती ने भले ही दलितों को अम्बेडकर पार्कों, हाथी और पार्टी के नीले रंग के अलावा कोई और ठोस मदद न भी की हो, दलितों के बीच अपना वोट प्रतिशत बढ़ा पाने में सफल हुई थीं। तो क्या लॉकडाउन में भी तमाम तकलीफों के बावजूद राम मंदिर, धारा-370 और ‘समान नागरिक संहिता’ का झुनझुना काम कर गया? जो भी हो, इतना तो पक्का है कि हमारी राजनीतिक जमातें अपने-अपने ‘कच्चे माल’ यानि समाज से कोसों दूर बैठी हैं। यह दूरी समाज में एक तरह का राजनीतिक शून्य पैदा करती है और नतीजे में समाज उन संकटों की राजनीतिक अभिव्यक्ति तक नहीं कर पाता जो उसे अहर्निश तकलीफ देते रहते हैं, संकटों पर गोलबंद होना तो दूर की बात है। नब्बे के दशक की शुरुआत में आए भूमंडलीकरण ने और कुछ किया हो, न किया हो, तीस फीसद आबादी का ऐसा एक शहरी मध्यमवर्ग जरूर खड़ा कर दिया है जिसे अपने अलावा किसी की कोई परवाह नहीं रहती। डर है, हमारी कलाएं, साहित्य और राजनीति कहीं इसी के लपेटे में न आ जाएं।


































राजनीती समाज से जुड़ने के बजाय, समाज को खुद से जोड़ रही है, आजकल की सामाजिक संस्थाएं अपने लोगो के हित में आवाज बुलंद करने के बजाय राजनीतिक संगठन को मजबूत करने का काम करते है पता नहीं हमारा सामाजिक ढाचा चुने हुए लोगो की चाटुकारिता क्यों करती है, इनसे सवाल नहीं होते हर कोई बस इनके समक्ष विनम्र मूर्ति बना रहता है।