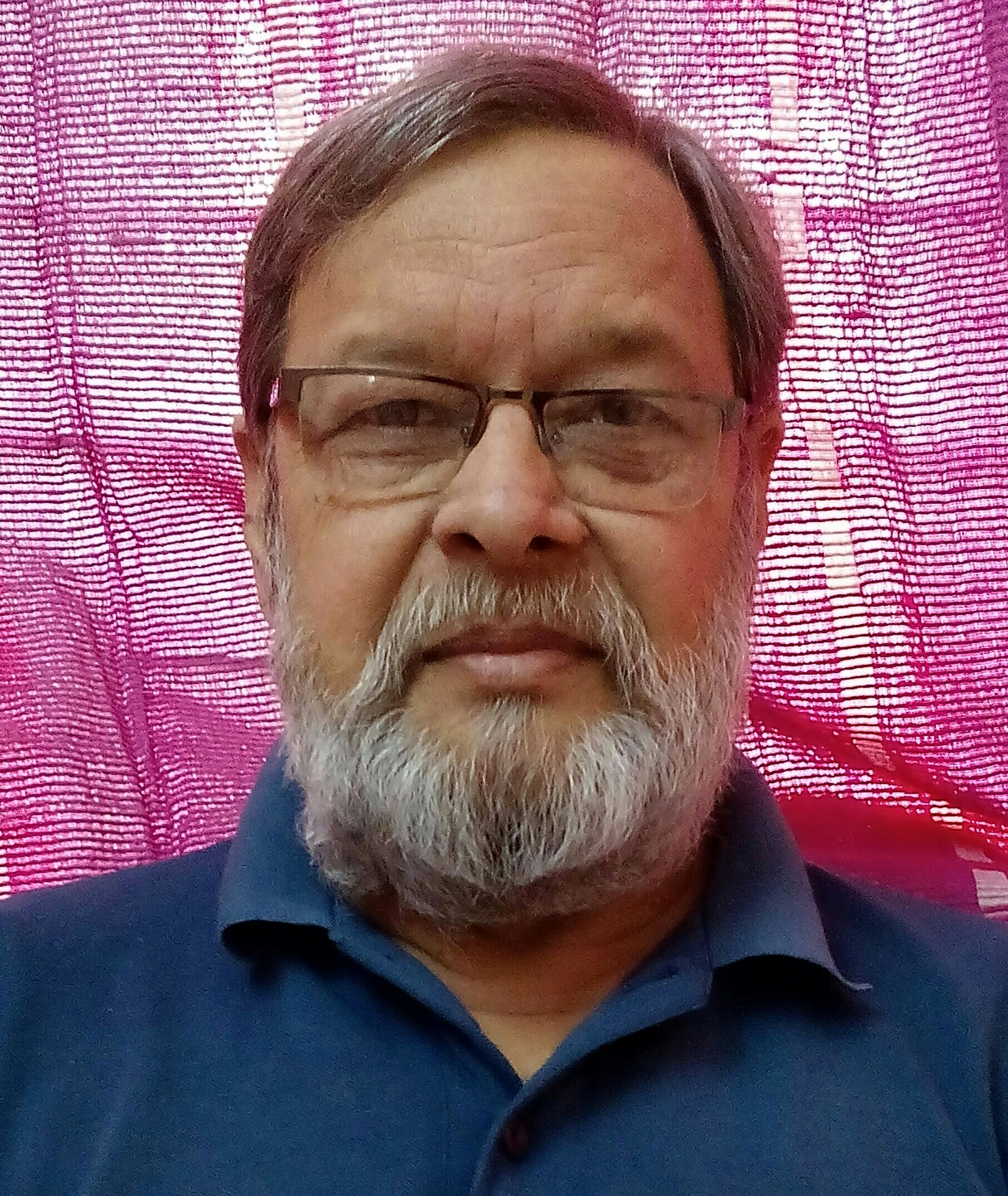
किसान आंदोलन पर भी शिद्दत और नासमझी से सवाल उठाया गया है कि लाखों लोगों के भोजन (लंगर) और दूसरी व्यवस्थाओं का इंतजाम आखिर कैसे और कौन कर रहा है? कुछ अधिक ‘कल्पनाशील’ शहरी इसमें कनाडा, इंग्लेंड, अमरीका और वहां बसे सिक्ख संगठनों, खासकर अलगाववादी संगठनों का हाथ देखने लगे हैं। अपने घरों में एकाध मेहमान को एकाध दिन ठहराने में जिन लोगों की दम निकल जाती है वे लाखों लोगों को शानदार लंगर खाते-खिलाते देखकर हतप्रभ तो होते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद वे किसान के मन की थाह लेना जरूरी नहीं समझते।
देश की राजधानी में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सरकार, बडी-छोटी-मझौली अदालतें और बडे-छुटभइए राजनेता आए दिन जो कहते-बताते रहते हैं उसमें क्या उनका शहरी मध्यमवर्ग ‘बोलता’ सुनाई नहीं देता? क्या पिछली सदी के नब्बे के दशक की शुरुआत में लाए गए भूमंडलीकरण की मेहरबानी से पनपा, फला-फूला शहरी मध्यवर्ग अपनी कुछ साल पहले की खेतीहर बुनियाद को भूलकर इतना गाफिल हो सकता है कि उसे किसान आंदोलन में केवल ‘विदेशी फंड’ और आतंकवाद भर दिखाई दे? या जिसे उदारता की पींग में महिलाओं, बूढों और बच्चों को आंदोलन से अलग करते हुए उन्हें वापस घर भेजना सुहाता हो? जबकि कमाई करने वाली 80 प्रतिशत महिलाएं खेती-किसानी में लगी हों और खेती का 75 फीसदी काम सम्भाल रही हों?
शहरी मध्यवर्ग और उसकी चापलूसी में लगी राजनीति, मीडिया और उनके दाएं-बाएं का समाज मानता है कि किसानी, उनके काम-धंधों की तरह मुनाफा कूटने और तमाम तरह की सरकारी सब्सीडी, कर-मुक्ति आदि का लाभ उठाने वाला एक आमफहम ‘सेक्टर’ है। यह मान्यता लगभग वैसी ही है जैसी झुग्गी बस्तियों को लेकर कही-बताई जाती है। झुग्गी बस्तियों के रहवासी इसी शहरी मध्यमवर्ग के नजरिए से नगर-सौन्दर्य पर बदनुमा दाग माने जाते हैं। अपने हितों, स्वार्थों की हुलफुलाहट में उन्हें याद ही नहीं रहता कि झुग्गी बस्तियों में उनके घर, काम-धंधे, स्कूल-कॉलेज और समूचा शहर चलाने वाले लोग रहते हैं। कुछ घंटों की इनकी हडताल खाते-पीते, खुशनुमा शहरों को घुटनों पर ला सकती हैं। शहरी मध्यमवर्ग की ऐसी मान्यताएं आखिर क्यों बनती हैं?

अव्वल तो इसकी वजह वह शिक्षा और समझ है जिसके चलते दाल-रोटी की खातिर शहरों में पहुंचा मध्यमवर्गीय आदमी अपने ग्रामीण, किसान पुरखों को पिछडा, अशिक्षित, गंवार और न जाने क्या-क्या कहने-मानने लगता है। शहर और गांवों के भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की भिन्नता के चलते बना शहरी और ग्रामीण मन का ताना-बाना और उसकी भिन्नता उसे समझ ही नहीं आती। दरअसल इस तरह की तमाम बातें शहरी मध्यवर्ग की अपनी जडों से लगातार बढती ऐसी दूरी दर्शाती हैं जिसका अंदाजा खुद शहरी मध्यमवर्ग को भी नहीं होता। इन दूरियों के चलते सबसे पहले सर्वाधिक चर्चित सवाल उठता है – धन या ‘फंड’ का।
किसान आंदोलन पर भी शिद्दत और नासमझी से सवाल उठाया गया है कि लाखों लोगों के भोजन (लंगर) और दूसरी व्यवस्थाओं का इंतजाम आखिर कैसे और कौन कर रहा है? कुछ अधिक ‘कल्पनाशील’ शहरी इसमें कनाडा, इंग्लेंड, अमरीका और वहां बसे सिक्ख संगठनों, खासकर अलगाववादी संगठनों का हाथ देखने लगे हैं। अपने घरों में एकाध मेहमान को एकाध दिन ठहराने में जिन लोगों की दम निकल जाती है वे लाखों लोगों को शानदार लंगर खाते-खिलाते देखकर हतप्रभ तो होते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद वे किसान के मन की थाह लेना जरूरी नहीं समझते।
पहले के अनेकों में से एक उदाहरण ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’ का भी है जिसके अनेक में कुछ उदाहरण काबिल-ए-गौर हैं। आंदोलन की एकदम शुरुआत में खंडवा जिले के हरसूद कस्बे में सितम्बर 1989 में ‘संकल्प मेले’ का आयोजन हुआ था। किसी व्यवस्थागत् खामी के चलते कार्यक्रम के ठीक दो दिन पहले तैयारी करने वालों को पता चला कि उनकी गांठ में एक पैसा नहीं है। अब करीब एक लाख लोगों को खिलाने-पिलाने, नहाने-धोने और सुलाने की व्यवस्था करवाने वालों के हाथ-पांव फूलना ही थे, लेकिन इस संकट से निजात दिलवाने में पंद्रह हजार आबादी वाले मामूली हरसूद कस्बे ने बढ-चढकर मदद पहुंचाई। करीब तीन घंटों में हरसूद के नागरिकों ने अस्सी हजार रुपए इकट्ठा करके यह कहते हुए कार्यकर्ताओं को सौंपे कि और जरूरत हो तो बताना, हम वह भी ‘उगा’ देंगे।
‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’ की साढे तीन दशक की लडाई में ऐसे अनेक अनुभव हैं जब किसी शहर, महानगर में धरना दे रहे लोगों को पैसा-धेला, रसद और अन्य जरूरत की चीजें आंदोलन के ग्रामीण-आदिवासियों ने पहुंचाई हैं। भोपाल का वह महीने भर का धरना-अनशन ख्यात है जब रोज करीब हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था निमाड के गांवों से होती रही। ‘सरदार सरोवर’ की डूब में बिना पुनर्वास डुबोए गए सैकडों आदिवासी परिवारों को महीनों राशन एवं अन्य जरूरत का सामान भेजा जाता रहा। किसानों के मन की यह उदारता और अपने साथियों को सहयोग देने का जज्बा शहर के मध्यमवर्गीय समाज को दिखाई नहीं देता।
दिल्ली के धरने में चूंकि सभी आंदोलनकारियों को भोजन और जरूरत का अन्य सामान सहजता से उपलब्ध करवाया जा रहा है इसलिए कहा जाने लगा है कि यह किसानों की बेहतरीन आय का नतीजा है। क्या सचमुच यह बात सही है? अव्वल तो आंकडों के मुताबिक देश के 68 फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास एक हैक्टेयर यानि ढाई एकड से कम जमीन है। किसान बिरादरी के कुल 86 प्रतिशत लोग ‘सीमान्त’ (एक हैक्टेयर) और ‘छोटी’ (दो हैक्टेयर यानि पांच एकड) जोत के मालिक हैं। जाहिर है, इतनी कम जमीन में उनका गुजारा नहीं हो पाता और उन्हें मजदूरी के भरोसे अपनी भूख मिटानी पडती है।
‘नाबार्ड’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3.36 लाख करोड रुपयों की सब्सीडी (खाद, बीज, बिजली, ‘एमएसपी’ आदि सभी मदों पर) के बावजूद देश के हरेक किसान पर औसतन एक लाख रुपयों का कर्ज चढा है। हालांकि ठीक इसके विपरीत उद्योगों को विभिन्न मदों में दस लाख करोड रुपयों की छूट दी जाती है। जाहिर है, दिल्ली धरने का इंतजाम छोटे, सीमान्त और कुछ बडे, लेकिन एकजुट किसानों की दम पर हो रहा है। किसानी मन की उदारता के अलावा इसमें सिक्ख, इस्लाम सरीखे धर्मों की वे परंपराएं भी शामिल हैं जिनके मुताबिक हरेक धर्मावलंबी के लिए अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा समाज के काम में लगाना होता है। असल में जरूरी है, अपने समाज को समझना और इसके लिए गाहे-बगाहे होने वाले अहिंसक, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक आंदोलन बेहद कारगर ‘कक्षाएं’ हो सकती हैं। दिल्ली का मौजूदा किसान आंदोलन इस लिहाज से भी बेहद जरूरी है।(सप्रेस)
































