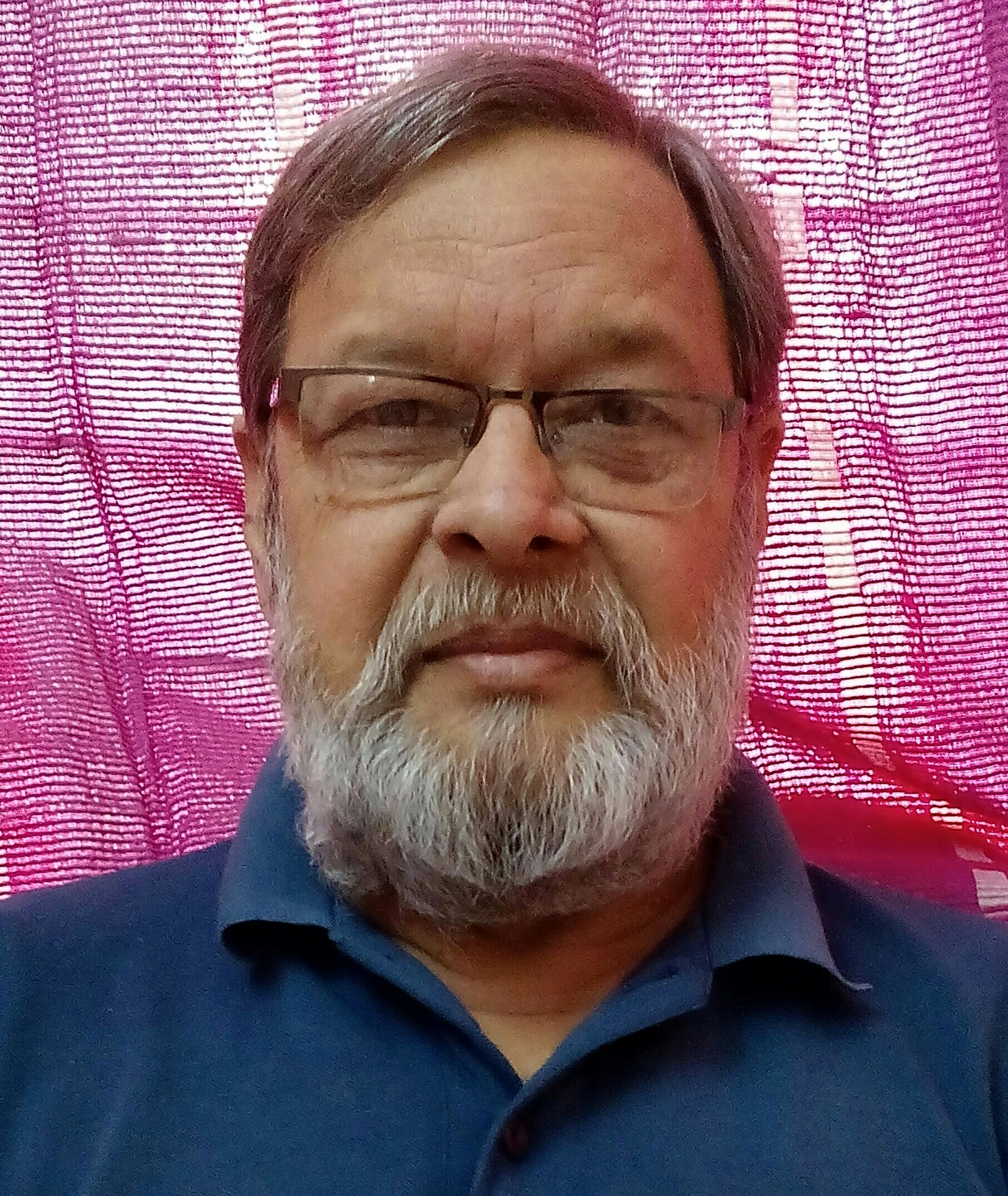
सवाल है कि क्या आज की बदहाली के लिए, खासतौर पर भारत में, लघु और विशाल के बीच का द्वंद्व ही जिम्मेदार है? क्या आजादी के बाद गांधी के लघु और उपयुक्त को नजरअंदाज कर बनाई गई ‘बिगेस्ट इन द वर्ल्ड’ की विशालकाय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक योजनाओं में ही कोई खोट है जिसने हमें मौजूदा बदहाली की तरफ ढकेल दिया है?
गोस्वामी तुलसीदास की ‘रामचरितमानस’ में एक प्रसंग है, राक्षसी सुरसा का। रावण की लंका में कैद जानकी को राम का संदेश देने जा रहे हनुमान की शक्ति-परीक्षा करने के लिए देवताओं ने सर्पों की माता सुरसा को भेजा था। तुलसी बाबा कहते हैं कि – ‘जस-जस सुरसा बदन बढावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जोजन तेहिं आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा।’ यानि पहले तो सुरसा से दुगना आकार ग्रहण करके हनुमान ने अपनी अहमियत दिखाई, परन्तु अंत में वे ‘अति लघु रूप’ में ही सुरसा से निपट पाए।
दुनियाभर में वापरी जाने वाली ‘उपयुक्त तकनीक’ यानि ‘एप्रोप्रिएट टैक्नॉलॉजी’ को सर्वप्रथम रेखांकित करने वाले अर्थशास्त्री ईएफ शूमाकर ने भी अपनी ख्यात किताब का नाम ‘स्मॉल इज ब्यूटीफुल’ यानि ‘लघु ही सुन्दर है’ रखा था। बौद्ध अर्थशास्त्र के ‘मज्झिम निकाय’ यानि ‘मध्यमार्ग’ से प्रभावित और तत्कालीन बर्मा सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे शूमाकर लघु को सुन्दर ही नहीं, कारगर भी मानते थे। शूमाकर ने अपने विचारों पर गांधी के प्रभाव को माना था जो खुद भी अपने जीवनभर छोटे और उपयुक्त के तरफदार रहे थे। सवाल है कि क्या आज की बदहाली के लिए, खासतौर पर भारत में, लघु और विशाल के बीच का द्वंद्व ही जिम्मेदार है? क्या आजादी के बाद गांधी के लघु और उपयुक्त को नजरअंदाज कर बनाई गई ‘बिगेस्ट इन द वर्ल्ड’ की विशालकाय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक योजनाओं में ही कोई खोट है जिसने हमें मौजूदा बदहाली की तरफ ढकेल दिया है?
तुलसीबाबा और शूमाकर की मान्यताओं को हमारे लोकतंत्र, आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक विकास और तरह-तरह के राजनीतिक-सामाजिक ढांचों की बदहाली के बरक्स देखें तो क्या पता चलता है? क्या आजादी के बाद स्थानीय, लघु और कारगर ताने-बाने को अनदेखा करते हुए विशालता की तरफदारी में बनाई गई योजनाओं ने हमारी मौजूदा गत नहीं बनाई है? इन दिनों हम बाढ़ की सालाना त्रासदी में डूब-उतरा रहे हैं और यदि इसी का उदाहरण लें तो स्थानीय स्तर के छोटे और कारगर ढांचे बचे होते और उनमें वर्षा-जल रोक लिया जाता तो क्या बाढ़ के इतने बड़े संकट में फंसना पड़ता? क्या ये छोटे और नियंत्रित ढांचे पानी की स्थानीय आपूर्ति और सिंचाई के लिए सर्वथा उपयुक्त नहीं होते? क्या मौजूदा विशालकाय, केन्द्रीकृत जल-विद्युत परियोजनाएं अपने उद्देश्यों को पूरा करने में इस कदर नकारा साबित नहीं हुई हैं कि उनसे मामूली बाढ़-नियंत्रण तक नहीं हो पा रहा? बड़ी, विशाल परियोजनाओं के कई अलमबरदार अब भी मानते हैं कि बड़े बांध सिंचाई, जल-विद्युत उत्पादन और बाढ़-नियंत्रण का अचूक नुस्खा हैं, लेकिन आजादी के बाद अब तक बने करीब पांच हजार बड़े बांध अपनी इन्हीं बुनियादी जिम्मेदारियों को निभा पाने में नकारा साबित हुए हैं। अपने आसपास ही देखें तो कोई भी बता सकता है कि बड़े बांधों के पहले की बाढ़, भले ही बड़ी हो, लेकिन उतना नुकसान नहीं पहुंचाती थीं जितना अब होने लगा है। पहले जमाने में बाढ़ का पानी कहीं रुकता नहीं था, लेकिन अब बड़े बांधों की चपेट में आने के बाद से पानी कई-कई दिन बस्तियों में ठहरा रहता है और नतीजे में भारी नुकसान पहुंचाता है।
एक और बानगी अभी दो दिन पहले आए ‘सकल घरेलू उत्पाद’ (जीडीपी) के आंकडों से देशभर में मचे बवाल की भी है। इनके मुताबिक भारत का ‘जीडीपी’ अपनी पहली तिमाही में ही लुढ़ककर ‘ऋण-23.9 प्रतिशत’ पर पहुंच गया है। इस ‘लुढ़कन’ में उस ‘निर्माण क्षेत्र’ (50 प्रतिशत) का सबसे अधिक हाथ है जिसकी कसमें खाकर हमारे विकास-वादी सत्ताधारी वाह-वाही कमाते थे। इसके अलावा अप्रैल से जून के बीच बढी इस राष्ट्रीय बदहाली के मुकाबले एक और आंकडा है, मुकेश अम्बानी की सम्पन्नता का। ‘जीडीपी’ गिरने के ठीक इसी दौर में अकूत कमाकर अम्बानी दुनिया के पांचवें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पहले से ‘दूबरे’ और ‘कोरोना’ की मार में ‘दो अषाढ’ झेलने वाले भारत में कोई एक आदमी, भले ही वह कैसा और कितना भी ‘बलवान’ क्यों न हो, कैसे दुनियाभर के ‘टॉप’ पूंजीपतियों में जगह बना सकता है? यह कैसा लोकतंत्र और संविधान है जिसमें नागरिकों के देखते-देखते देश की ‘जीडीपी’ लुढकने के एन दौर में कोई अपनी संपत्ति में 35 फीसदी का इजाफा करके दुनिया के अमीरों की नंबर एक की दौड़ में शामिल हो जाता है? संविधान से बंधे लोकतांत्रिक देश के नागरिक क्या इस परिस्थिति में अपना कोई हाथ लगा सकते हैं? और क्या यह गफलत विशालकाय, राक्षसी के बरक्स लघु के विरोधाभास का ही नतीजा नहीं है?
इस लिहाज से देखें और पड़ताल करें तो सरलता से समझा जा सकता है कि हमारा और तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों का बुनियादी द्वंद्व ‘विशालता’ और ‘लघुता’ के बीच का है। इसे थोड़ी और गहराई से देखें तो लोकतंत्र और संविधान के विरोधाभासों को भी समझा जा सकता है। देश का संविधान हमें ‘क्या है’ की बजाए ‘क्या होना चाहिए’ तो बताता है, लेकिन हमारी मौजूदा हालातों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। मसलन, क्या हमारे संविधान में राज्य-राज्य में जारी मौजूदा शर्मनाक राजनीतिक उठा-पटक के लिए कोई जगह है? क्या संविधान हमारे राजनेताओं को वैसा बनने और बने रहने से रोक सकता है, जैसे कि वे हैं? और यदि यह सब नहीं है, तो फिर इससे कैसे पार पाया जा सकता है? लोकतंत्र और संविधान की श्रेष्ठतम उपलब्धि समाज के अंतिम नागरिक की तंत्र में भागीदारी मानी जाती है, लेकिन क्या मौजूदा राजनीतिक ताने-बाने में यह किसी भी तरह से संभव दिखती है? यदि ऐसा नहीं है तो फिर एक काल्पनिक, आभासी लोकतंत्र और संविधान की क्या भूमिका होगी? क्या ऐसे में नागरिक की पहुंच की न्यूनतम राजनीतिक इकाई ग्रामसभा को मजबूत करें तो अपेक्षित परिणाम नहीं पाए जा सकते? गांधी तो चीख-चीखकर इसी ग्राम गणराज्य की बात करते रहे थे।
ग्रामसभा को मजबूत और कारगर बनाकर बिगडैल राजनीतिक जमातों को रास्ते पर लाया जा सकता है, लेकिन हमारी राजनीतिक बिरादरी में इसके प्रति कोई लगाव नहीं है। इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में आए ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून’ (मनरेगा) या ‘वनाधिकार अधिनियम’ जैसे कानूनों ने पंचायतों और ग्रामसभाओं को पैसा और ताकत दी है। नतीजे में कतिपय राजनीतिक दल लोकतंत्र की इन लघुतम इकाइयों के प्रति थोड़े-बहुत आकर्षित भी हुए हैं, लेकिन यह आकर्षण पंचायतों, ग्रामसभाओं को मजबूत बनाने की बजाए उन्हें और कमजोर करने के प्रति है। आखिर मजबूत नागरिक और उनकी पंचायतें, ग्रामसभाएं मौजूदा राजनीति को कहां रास आती हैं। लेकिन आप चाहें, न चाहें, भविष्य तो इन्हीं का है।
थोड़ी गहराई से खंगालें तो साफ देखा, महसूस किया जा सकता है कि इंसानी वजूद के सभी क्षेत्रों में अब विशालता का समय समाप्त होता जा रहा है। बड़े बांधों से लेकर बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों तक सभी धीरे-धीरे अपनी चमक खोते, अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। खेती-पाती, रहन-सहन, इलाज-बीमारी, पढाई-लिखाई आदि सभी क्षेत्र अब स्थानीय, छोटे ढांचों में ज्यादा कारगर दिखाई देने लगे हैं। जिस तरह पानी के लिए बड़े, विशालकाय बांधों की जगह छोटी, कारगर जल-संरचनाएं उपयुक्त साबित हो रही हैं, ठीक उसी तरह प्रशासन, राजनीति और समाज-व्यवस्था भी स्थानीय, छोटे ताने-बाने में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी साबित हो रही हैं। यह समय है, जब हमें अपने मौजूदा ढांचे में पैबन्द लगाने की बजाए उसे बदलने पर विचार करना चाहिए। ऐसे में विशालकाय, राक्षसी के मुकाबले छोटे, स्थानीय ढांचों को तरजीह देना एक विकल्प हो सकता है।
































