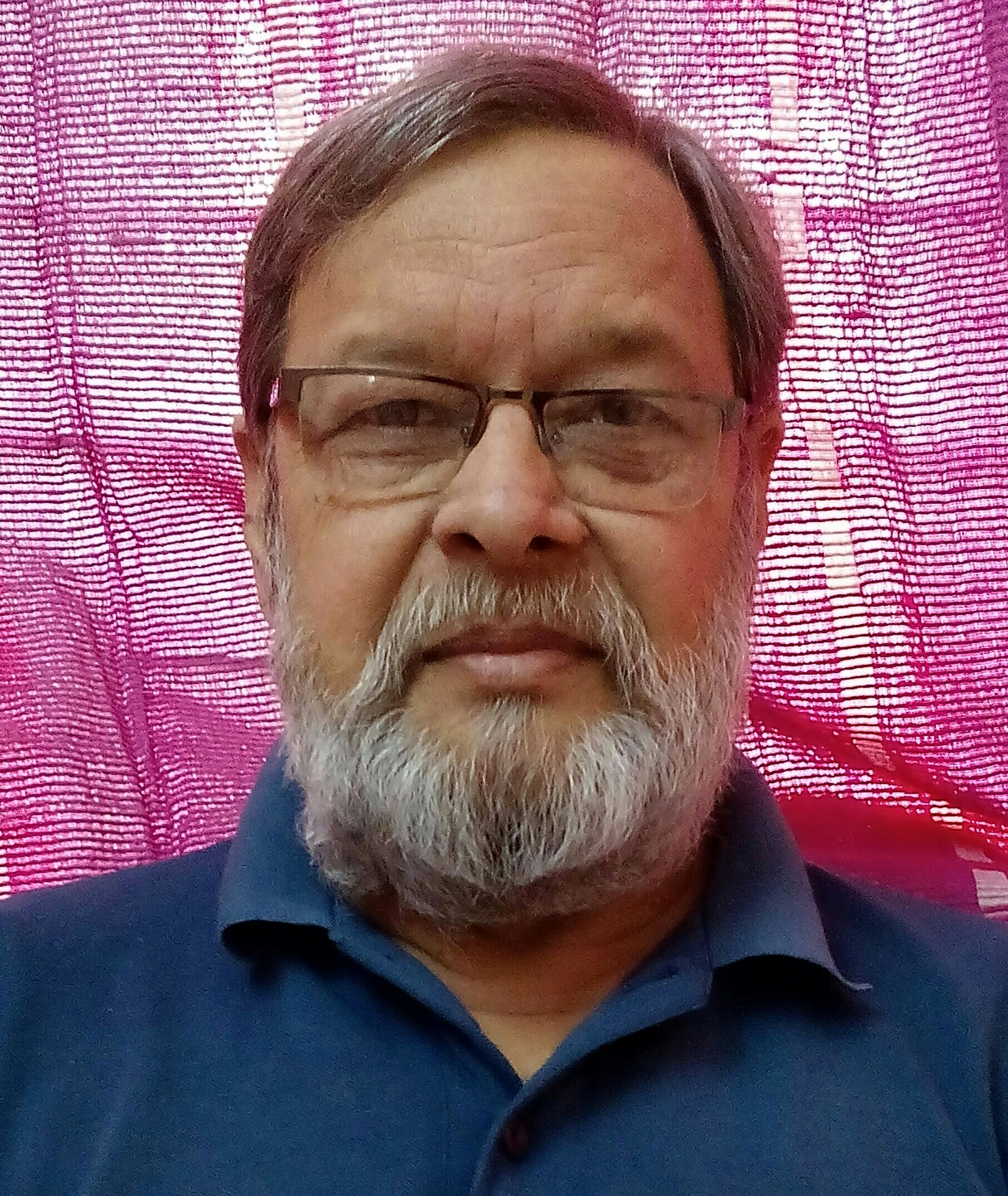
एन कोविड-19 के महामारी-काल में भीषण बेरोजगारी, भुखमरी और बीमारियों को सिरे से भुलाकर भारतीय मीडिया कंगना-रिया की चटखारेदार कहानी में रमा है। मानो देश के सामने अब कुल मिलाकर कंगना का टूटा दफ्तर और रिया की कथित नशे की आदतें भर कुल मुद्दे बचे हैं। क्या चहुंदिस ‘विकास’ के हल्ले के बावजूद मीडिया हमारे समूचे समाज में अपनी पैठ जमा पाया है? और यदि यह भूमंडलीकरण की कृपा से फले-फूले-फैले कुल आबादी के करीब तीस फीसदी शहरी मध्यमवर्ग की आदतों में शुमार हो गया है तो फिर बाकी के सत्तर फीसदी आम लोग कैसे जीते-मरते हैं? क्या उनके लिए, उनका भी कोई मीडिया है?
कंगना रानाउत और रिया चक्रवर्ती की चटखारेदार, सीरियल-नुमा कहानियों में डूबते-उतराते लोगों के लिए भले ही मीडिया मनोरंजन परोसने की एक फैक्ट्री की तरह स्थापित हो चुका हो, लेकिन क्या खबरों की अब हमारे संसार में कुल मिलाकर इतनी-भर हैसियत बची है? क्या खबरें और मनोरंजन अब ‘सहोदर’ हो गए हैं जिनमें किसी एक की बढौतरी, दूसरे को भी कई-कई गुना लाभ पहुंचा सकती है? पारंपरिक मार्क्सवाद में मीडिया की इस भूमिका को धर्म की तरह ‘अफीम’ माना जाता है। मीडिया की यह ‘अफीम’ नागरिकों को सम-सामयिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन से बेजार रखती है, ताकि पूंजी अपनी बेहूदी, बेहिसाब उडान भर सके। तो क्या ‘सास बहू’ के सोप-ऑपेरा से लगाकर कंगना-रिया के ‘रीयलिटी-शो’ तक पहुंचा भारतीय मीडिया अब कुल मिलाकर सिर्फ मनोरंजन दिखाने, सुनाने भर का कारखाना बन गया है?
एक तरह से देखें तो कंगना-रिया की कथा पूंजीवाद के विकास की मार्क्सवादी अवधारणा में फिट बैठती दिखती है। एन कोविड-19 के महामारी-काल में भीषण बेरोजगारी, भुखमरी और बीमारियों को सिरे से भुलाकर भारतीय मीडिया कंगना-रिया की चटखारेदार कहानी में रमा है। मानो देश के सामने अब कुल मिलाकर कंगना का टूटा दफ्तर और रिया की कथित नशे की आदतें भर कुल मुद्दे बचे हैं। लेकिन क्या इसे हम देशभर की समस्या मान सकते हैं? क्या चहुंदिस ‘विकास’ के हल्ले के बावजूद मीडिया हमारे समूचे समाज में अपनी पैठ जमा पाया है? और यदि यह भूमंडलीकरण की कृपा से फले-फूले-फैले कुल आबादी के करीब तीस फीसदी शहरी मध्यमवर्ग की आदतों में शुमार हो गया है तो फिर बाकी के सत्तर फीसदी आम लोग कैसे जीते-मरते हैं? क्या उनके लिए, उनका भी कोई मीडिया है? इन सवालों का जबाव खोजने के लिए हमें 1990 के दशक के बदलाव पर गौर करना होगा।
आजादी के बाद से जारी ‘मिश्रित अर्थव्यवस्था’ को ठेंगे पर मारते हुए नब्बे के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्तमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सदारत में भूमंडलीकरण का पदार्पण हुआ था। उस जमाने में खुले बाजारों वाली इस नीति की मान्यता थी कि बाजार, बिना सरकारी इमदाद और नियंत्रण के, अपनी चाल से, अपनी शर्तों पर चल लेगा। सब जानते हैं कि आज का मीडिया बाजार का पिछलग्गू है और भूमंडलीकरण में बाजारों के खुलते ही मीडिया ने भी तरह-तरह के सरकारी, सामाजिक नियंत्रणों को धता बताते हुए अपनी राह बनाना शुरु कर दिया। यही वह दौर था जब बाजार के प्रभाव में, एक फलते-फूलते बाजार की शक्ल में शहरी मध्यमवर्ग की हैसियत में इजाफा हुआ और नतीजे में मीडिया उसी की चाकरी को अपना सबसे अहम काम मानने लगा। यही वह समय था जब तरह-तरह के सीरियल, ‘सोप-ऑपेरा’ और रीयलिटी-शो बने, पनपे और खूब लोकप्रिय भी हुए।
अलबत्ता, इस सबको खडा करने वालों को ठीक पिछले दशकों में हुई कवि-सम्मेलनों की मिट्टी-पलीती दिखाई नहीं दी। साठ, सत्तर के दशकों में युवा रहे लोग जानते हैं कि उन दिनों कवि-सम्मेलनों की धूम हुआ करती थी और इक्का-दुक्का सिनेमाघरों के अलावा लोग भवानीप्रसाद मिश्र, गोपालदास ‘नीरज,’ सोम ठाकुर, देवराज दिनेश, शैल चतुर्वेदी, रमेश ‘रंजक,’ विनोद निगम, सुरेश उपाध्याय, माहेश्वर तिवारी आदि को ही देखने-सुनने का ‘क्रेज’ था। धीरे-धीरे कवि-सम्मेलन भी व्यवसाय बनते गए और साहित्यिक और लोकप्रियता के बीच की बहसों के अलावा हास्य और फूहडता की ओर बढते गए। ऐसे अनेक कवि-सम्मेलनों के उदाहरण हैं जिनमें खुद को ‘जमाने’ के लिए कवि अश्लील, फूहड, द्विअर्थी कविताएं सुनाते थे और कई बार तो बेशर्म शारीरिक हरकतें तक किया करते थे। जाहिर है, कवि-सम्मेलन अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे थे और उन्हें प्रासंगिक बनाए रखने की जद्दोजेहद में कवि भोंडे, अश्लील बनने तक को तैयार थे।
कवि सम्मेलनों की यही दुख भरी दास्तान आज के टीवी कार्यक्रमों, खासकर समाचारों की मार्फत दोहराई जा रही है। अस्सी और नब्बे के दशकों में टीवी के जरिए परोसा जा रहा गंभीर, सोद्देश्य और सकारात्मक मनोरंजन और समाचार धीरे-धीरे फूहड, अश्लील और निरुद्देश्य-निरर्थक कसरत में तब्दील होते जा रहे हैं। एन समाचारों में परोसी जा रही कंगना-रिया की चीखती हुई कहानियां असल में मीडिया, खासकर टीवी की बदहाली की कहानी बयां कर रही हैं। कहा भी जा रहा है कि समाचार चैनलों के मुकाबले ‘रीयलिटी शो’ से अधिक राजस्व कमाया जा सकता है और इसीलिए समाचार भी ‘रीयलिटी शो’ में तब्दील होते जा रहे हैं। तो क्या एक जमाने के कवि-सम्मेलनों की तरह अब टीवी समाचारों, सीरियलों की भी समाप्ति का समय आ गया है?
अव्वल तो शहरों की चौहद्दी के बाहर जो सत्तर फीसदी आबादी आबाद है, उसे मीडिया ने सप्रयास अपने धतकरमों से बाहर कर दिया है। यह सत्तर फीसदी आबादी उन तीस फीसदी शहरी मध्यवर्गीयों की तरह बाजार नहीं है कि अपनी तमाम वैध-अवैध बातों को मीडिया और दूसरे संस्थानों से मनवा ले। बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, विस्थापन जैसी व्याधियों से इसी सत्तर फीसदी को लगातार निपटते रहना होता है और मीडिया इसे दिखाने-पढाने से आमतौर पर परहेज ही करता है। कंगना-रिया की कहानियों के दौरान अभी दो दिन पहले हरियाणा के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर बेहद प्रभावी प्रदर्शन किया और देश के एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग को ठप्प तक कर दिया, लेकिन मीडिया में इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं हुई।
दूसरे, कोविड-19 की मेहरबानी से लगे लॉकडाउन ने पिछले पांच-छह महीनों में शहरी मध्यमवर्ग को भी सडकों पर ला दिया है। नब्बे के दशक के बाद के अपने ‘उत्थान’ के चलते खासी आरामतलब, अलिप्त और कभी-कभार सत्तानुरागी जिन्दगी जीने वाले शहरी मध्यमवर्गीय लोगों को भी अब बेरोजगारी, वेतन-कटौती और बदहाली से दो-चार होना पड रहा है। ऐसे में रीयलिटी-शो की तरह परोसी जाने वाली खबरें तक उनमें चिढ पैदा करती हैं। सवाल है कि क्या अपने ‘उपभोक्ताओं’ की इस बदहाली के चलते मीडिया वैसा ही रह पाएगा, जैसा वह आज है? यानि क्या कंगना-रिया के दर्जे की कहानियों को सुनने वाला कोई ग्राहक मिलेगा? खासकर तब, जब सोशल-मीडिया खबरों के एक अखंड स्रोत की तरह स्थापित हो गया हो?
तमाम विज्ञापनों, ‘पेड-न्यूज,’ और भूत-प्रेत से लगाकर भगवानों तक की मार्फत ‘राजस्व’ कूटने वाले मीडिया के लिए भी समाचार, जानकारियां और सूचनाएं देना एक प्रकार की जन-सेवा माना जाता है। इसे निर्बाध चलाए रखने के लिए विज्ञापनों के जरिए राजस्व उगाना जरूरी है, लेकिन यह किसी हालत में केवल पैसा बनाने की प्रक्रिया नहीं हो सकती। आज के दौर में पूंजी बनाने की हुलफुलाहट में समाचार भी मनोरंजन की श्रेणी में आ गए हैं। ऐसे में मीडिया पर नियंत्रण के लिए पारंपरिक ‘स्व-नियमितीकरण’ यानि ‘सेल्फ-रेगुलेशन’ की एक तरकीब मौजूद है, हालांकि इस ‘नख-दंतहीन’ प्रक्रिया का कोई पालन नहीं करता। एक और तरीका मीडिया से ‘अघाने’ का भी है जिसे पश्चिम के कई देशों में अब महसूस किया, देखा जा रहा है। यानि एक ही तर्ज-तरकीब से लगातार चलने वाले मीडिया को देख-देखकर लोग ऊब जाते हैं और नतीजे में मीडिया को खारिज कर देते हैं। भारत में ये तरकीबें कितनी कारगर होती है, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन मीडिया को खुद अपना भविष्य देखने की आदत डाल लेनी चाहिए। ऐसा न हो कि सत्तर फीसदी आबादी से दूर बैठा मीडिया अपने तीस फीसदी शहरी मध्यवर्ग के ग्राहकों की नजरों से भी उतर न जाए?
































