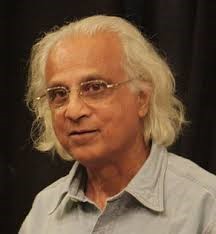
जिस तेजी से शहरों के विकास हो रहे हैं, उसने नगर-नियोजन की अहमियत कई गुना बढ़ा दी है। इसमें उस आबादी का खास महत्व है जो आसपास के गांव-खेडों से रोजगार की आस में शहरों की तरफ खिंची चली आती है। ऐसे में कैसी होगी बसाहट? क्या मौजूदा पद्धति से शहरों का नियोजन कारगर साबित हुआ है?
शहरी नियोजन का सफरः
हम सब अपने कामों से सीखते हैं। कोई भी सिखाने की कोशिश करे फिर भी जब तक खुद अनुभव नहीं करते तब तक हमेशा एक दुविधा और अविश्वास की स्थिति बनी रहती है। करीब 50 साल पहले हमारी टोली अनूपपुर कस्बे में पहुंची थी। उसके पहले चार साल तक हमने देश के विभिन्न हिस्सों के विकास कार्यों में हिस्सा लिया था। तमाम सरकारी, गैर-सरकारी समाजसेवी और विकासोन्मुखी संस्थाओं को काम करते हुए देखा था। नतीजे में दो सवाल उठे। ‘विकास किसे कहते हैं?’ और ‘आम लोग अपना विकास कैसे कर सकते हैं?’
बुच साहब का काम और उनके सबकः
स्व. एमएन बुच की नगर-नियोजन की सीख से भी बड़ा सबक था कि इंसान गलती करके ज़्यादा समझता है। भोपाल Bhopal की 1991 की विकास योजना 1975 में बनवाने में उनका बड़ा हाथ था, लेकिन 1992 में उन्होंने अपनी ही योजना की आलोचना करते हुए कहा था कि जब ज़मीन का एक बार शहरीकरण हो जाता है तो वह अपनी प्राकृतिक गुणवत्ता खो देती है और इस बदलाव की कीमत कभी आंकी नहीं जाती। अपनी किताब ‘व्हेन द हार्वेस्ट मून इज ब्ल्यू’ में उन्होंने लिखा कि यदि सरकारी अधिकारी अपना घमंड त्याग दें तो उन्हें देश के नागरिकों से मिलकर पूरे संसार के बारे में सीखने का अनमोल अवसर मिल सकता है। 1986 में तैयार ‘शहरीकरण के राष्ट्रीय आयोग’ (जिसके वे सदस्य थे) की रिपोर्ट का विश्लेषण उन्होंने 30 वर्ष बाद करते समय स्वीकारा कि बाजार के रास्ते शहर के नवीनीकरण की नीति को नेहरू (जेएनएनयूआरएम), स्मार्ट शहर और इकोसिटी जैसे मिशन ने झुठला दिया है।
भोपाल का भूगोलः
भोपाल को गोंड रानी ने स्थापित किया या राजा भोज ने – इस पर बहस होती रहेगी, लेकिन उसके भूगोल पर कोई विवाद नहीं है। महानगर के पश्चिम में पहाड़ी इलाका है जिसमें बरसाती पानी को संजोया जा सकता है। पूरब में जंगल और उपजाऊ ज़मीन है और इसी में नगर का विस्तार हुआ है। भोपाल से दो रेल-पटरियां और छह राजमार्ग गुज़रते हैं जिनकी वजह से इसे क्षेत्रीय विकास का ध्रुव माना गया है, लेकिन बुच साहब के विचारों के मुताबिक क्या इस विकास से पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा हो पायी? नहीं तो बाघ, तेंदुआ जैसे जंगली जानवर शहर के रहवासी क्षेत्रों में क्यों धावा बोल रहे हैं? नगर के विस्तार से भीड़ कम होनी चाहिए, लेकिन देखने को मिलता है कि निर्माण कार्य रुक नहीं रहा है; और तंगी भी लगातार बढ़ती जा रही है।
नियोजन का इतिहासः
वर्ष 1956 में भोपाल को मध्यप्रदेश की राजधानी का दर्जा मिला और 1959 में नगरीय विकास की नींव रखी गयी। योजना के अनुसार पुराने शहर के दक्षिण में नया शहर बनने लगा। सचिवालय का निर्माण हुआ, मंडियों को पुराने शहर से बाहर निकाला गया और धरोहर की रक्षा की व्यवस्था हुई, लेकिन 1971 तक उत्तर में ‘यूनियन कार्बाइड’ फैक्टरी और पूरब में ‘भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स’ के विशाल परिसर बन गए। 1974 में बुच साहब ने नगर नियोजन और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी संभाली। उनकी देख-रेख में ‘भोपाल विकास योजना 1991’ तैयार हुई जिसमें तालाब और जंगल को बचाने की कोशिश की गयी। 1995, 2011 और 2023 में भी योजनाएं बनीं, लेकिन शहर फैलता गया और जल, जंगल, ज़मीन समाप्त होते गए।
मूल्यांकनः
नियोजन का पहला सिद्धांत है, पिछली कोशिशों पर नज़र दौड़ाएं। मसलन, जब 1995 में 2005 तक की योजना बनने लगी तब पाया गया कि उसके पहले 20 वर्षों में दो तिहाई से तीन चौथाई ज़मीन का ही उपयोग हो पाया था, लेकिन उस ज़मीन पर क्या बना इसका कोई ज़िक्र नहीं हुआ। 2005 की योजना के मूल्यांकन में अधिकांश इकाइयाँ नहीं बनी, लेकिन क्यों नहीं बनीं, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। और तो और, ज़मीन का उपयोग ना होते हुए भी, अगली योजना में और अधिक ज़मीन की मांग कर दी गयी! खास बात यह रही कि अन्य कानूनों और परियोजनाओं का नगर नियोजन पर क्या असर पड़ा, इस पर विचार का अभाव रहा। कुछ कानून हैं जो जनपक्षीय हैं, बाकी योजनाएं हैं जो बाजार-हितैषी हैं। इसलिए यह भी समझना ज़रूरी है कि कानून और नीति बनाते कौन हैं और उनका नजरिया क्या है?
सर्वेक्षण और उपयोगिता:
दूसरा सिद्धांत है, शहर का विस्तृत सर्वेक्षण करके वर्तमान हालात और ज़रूरतों को आंकना। कितनी आबादी क्या कर रही है; रोटी-कपड़ा-मकान की क्या स्थिति है; लोगों की क्या उम्मीदें हैं? इस जानकारी के आधार पर तय हो सकता है कि किस सुविधा की कितनी ज़रूरत है और किस वर्ग को प्राथमिकता दी जाये। 1966 के सर्वे में देखा गया था कि सड़क पर सबसे अधिक पदयात्री थे। 1961 और 1971 की गणना के मुताबिक सबसे अधिक रोजगार छोटे-छोटे उद्योगों में मिलता था। उन्हीं दो वर्षों और 2001-2011 के आंकड़े बताते हैं कि कच्चे और छोटे घरों की संख्या अधिक थी। क्या योजनाकारों ने नियोजन के नियमों का पालन करके इन वर्गों पर ध्यान दिया? या गाड़ी, बड़ी फैक्टरी और पक्के मकानों को ही केंद्र में रखा? योजनाकार क्या पैदल, मज़दूर और छोटे, कच्चे घरों में रहने वाले होते हैं?
मानक और लोगों में वर्गीकरणः
मूल सामाजिक असमानता के विषय में नियोजन का कोई सिद्धांत नहीं है। उदाहरण के लिए 2005 की योजना में मनोरंजन के मानक दिये हुए हैं। उनसे स्पष्ट हो जाता है कि खेल के मैदानों और पार्कों की सुविधाओं तक, दूरी के कारण पैदल जाना नामुमकिन है। वहाँ पहुँचने के लिए वाहन चाहिए। यह छिपी हुई वर्ग व्यवस्था आवास, रोजगार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सफ़ाई, पर्यावरण – हर क्षेत्र में दिख जाती है। जो ‘स-धन’ है उसी को साधन मिलेगा। यही बाजार-हितैषी नज़रिया है। निजीकरण और कौशल के बीच एक काल्पनिक कड़ी बनाई गयी है। पहले हम नागरिक थे, जिनको अधिकार था, लेकिन अब हम सब ग्राहक बन गए हैं जो कल्याणकारी अधिकारी पर निर्भर हैं।
भेद-भाव के बीच का पुलः
अदृश्य असमानता को उजागर करने वालों की तेज़ आलोचना की वजह से नीति निर्धारकों ने एक नये सिद्धांत का आविष्कार किया। इसे कहते हैं – रिसन (ट्रिकल डाउन)। समाज में तीन वर्गों को पहचानते हुए इस सिद्धांत के अनुसार जब ऊपरी वर्ग में धन का निवेश होता है तब वह विकास कहलाता है। माना जाता है कि इससे रोजगार बढ़ेगा; कमाई बढ़ेगी। फिर लोग बाजार से सामान खरीद पाएंगे और विकास होगा। विकास धीरे-धीरे रिसते हुए निचले वर्ग तक पहुंचेगा। जहाँ इस रिसन का सबूत नहीं मिलता, वहाँ लक्षित वर्ग को नगद भुगतान की बात की जाती है, लेकिन उसके मानक कम होते हैं। नियोजन में पहले भागीदारी का आदर्श था, जिसकी जगह चयनित परामर्श ने ले लिया है।
विकास का इंजन और स्थान का वर्गीकरणः
नियोजन का चौथा सिद्धांत है, जिस शहर में अधिक सुविधाएं हैं उस शहर को अव्वल नंबर का माना जायेगा। शहर में यदि अधिक निवेश होता है, तो दूसरे छोटे शहरों को उससे जोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि विकास की तरंगें मूल शहर से फैलेंगी तथा धीरे-धीरे पूरा क्षेत्र विकसित हो जायेगा। इसी के तहत भोपाल विकास का इंजन है और विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास इत्यादि उसके डब्बे। इस कल्पना का पहला वर्णन आठवीं ‘पंच-वर्षीय योजना’ में मिलता है और 1990 में विश्वबैंक और ‘अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष’ द्वारा लागू आर्थिक सुधारों से जुड़ा हुआ है। गांवों से उजाड़े गए गरीबों का शहर की तरफ रोज़गार की तलाश में कूच करना भी इससे सम्बंधित है।
चतुर्मुखी विकासः
ये चार वर्गीकृत सिद्धांत दिखने में बड़े खूबसूरत हैं। मध्यम वर्ग जी-जान से मानता है कि सरकार या निजी निवेशकों द्वारा अमीरों को धन देने से गरीबों का भी भला होगा और पूरे देश में विकास के फायदे पहुंचेंगे। सवाल है कि आखिर ‘निवेशकों के पास धन आएगा कहाँ से?’ और ‘गरीब शहर में आकर भी गरीब क्यों रह जाते हैं?’ अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, प्रवासी मज़दूर गांव से शहर में आकर 4 से 6 गुना अधिक काम करते हैं, लेकिन वेतन लगभग उतना ही पाते हैं। जाहिर है, धन नीचे से ही बटोरा जाता है। अर्थात विकास रिसता नहीं, बल्कि सोख्ते का काम करता है। सोखने के बाद मुनाफा ऊँचे वर्ग के पास ही पहुँचता है और फिर निवेश के रूप में प्रकट होता है, और धन सोखने के लिए।
श्रमिक योजनाः
अनुभवों से हमें पता चला कि निचला वर्ग ही सोख्ते को रोककर वैकल्पिक सोच को सामने रख सकता है। भोपाल की 2031 की विकास योजना बताती है कि शहर में कई ‘मलिन बस्तियां’ हैं। इन स्व-निर्मित बस्तियों में शहर की व्यवस्था को चलाने वाले मजदूर रहते हैं। अर्थात ‘भू-उपयोग’ की जगह वे शहर के ‘श्रम-उपयोग’ को दर्शा रहे हैं। क्या इसको पहचानकर मेहनतकशों को सम्मानित किया जा सकता है? प्रत्येक बस्ती के इर्द-गिर्द दो किलोमीटर का घेरा बनाकर उसे नियोजन क्षेत्र माना जाए। उसी क्षेत्र में रोजगार, आवास, पैदल, सायकल और सभी सुविधाओं का विकेंद्रीकृत आयोजन हो सकता है। जहाँ अधिक मजदूर बस्तियाँ हैं उन्हें बाकी शहर में जगह मिल सकती है, लेकिन ऐसे दुरुस्त इंतेज़ाम के लिए एक अलग ही नज़रिया चाहिए।
क्या मजदूर वर्ग योजना बना सकता है?
यह प्रश्न पूछने वालों से प्रतिप्रश्न पूछना लाज़मी है, ‘क्या वह महिला जो ₹250 की न्यूनतम दिहाड़ी पर अपने परिवार की परवरिश कर सकती है, अपने पड़ौस की देखभाल करना नहीं सीख सकती?’ इस प्रश्न के संदर्भ में हम एक उदाहरण पेश करना चाहेंगे। अनूपपुर में काम करते समय हमने एक टुकड़ा ज़मीन खरीदी थी। कुछ दिन में पडौसी झगड़ने आ गए कि हमने ज़्यादा ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। चूंकि हमारे पास नापने वाली जरीब थी और नापना भी आता था तो हमने उनके सामने नापकर दिखा दिया कि हमने कम ही ज़मीन घेरी थी।
अगले दिन पास के गांव के कुछ छोटे किसान आये और उन्होंने आग्रह किया कि हम उन्हें ज़मीन नापना सिखा दें। चार दिन में हमने उन्हें थोड़ा बहुत सिखा भी दिया। जिस दिन पटवारी उनके गांव आया उस दिन वे हमसे जरीब मांगकर ले गए। कौतूहलवश हमने दूर से देखा कि जहाँ पटवारी अपनी जरीब खींच रहा था वहीं किसान भी मांगी हुयी जरीब खींचकर अपनी पुस्तिका में लिखते जा रहे थे। अगले दिन वे जरीब लौटाने आये तो बड़े खुश थे, परन्तु अपनी पुस्तिका दिखाने से हिचक रहे थे। जब दिखाई तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं था! हमारे चेहरे देखकर वे बोले, ‘बरसों से हमें नहीं मालूम था कि पटवारी क्या करता है, आज पहली बार पटवारी को मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे थे!’ ऐसे अनुभवों से ही शहर के जन-नियोजन का मूल मन्त्र और तंत्र समझा जा सकता है! (सप्रेस)































